पाठ्यक्रम: GS1/संस्कृति
संदर्भ
- हाल ही में राजभाषा विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो 1975 में इसकी स्थापना के 50 वर्षों को चिह्नित करती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित किया, यह कहते हुए कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि ‘राष्ट्र की आत्मा’ है।
भारतीय भाषाओं के बारे में
- भारत की भाषाई विविधता केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं — यह उसकी राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक भावना और समावेशी विकास की आधारशिला भी है।
- सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत: जनगणना 2011 ने 121 भाषाओं को मान्यता दी और सम्पूर्ण भारत में 1,600 से अधिक मातृभाषाएँ प्रचलित हैं।
- सिंधु घाटी लिपि, ब्राह्मी और खरोष्ठी भारत की दीर्घकालीन साहित्यिक परंपराओं को दर्शाने वाली प्रारंभिक लिपियों में शामिल हैं।
- भारत की ग्यारह मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषाएँ हैं — तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और हाल ही में जोड़ी गई मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला।
- संवैधानिक और कानूनी मान्यता: भारत का संविधान आठवीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को मान्यता देता है, जो क्षेत्रीय भाषाओं की समान स्थिति और प्रोत्साहन को सुनिश्चित करता है।
- अनुच्छेद 350A के तहत राज्यों को अल्पसंख्यक भाषाई समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
- संविधान भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी देता है।
- अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है, साथ ही अंग्रेज़ी का प्रयोग भी जारी रखने की अनुमति है।
- अनुच्छेद 344 राजभाषा के उपयोग की प्रगति की समीक्षा और अनुशंसा हेतु एक आयोग और समिति के गठन की व्यवस्था करता है।
- अनुच्छेद 345 राज्य विधानमंडलों को राज्य में प्रयुक्त किसी भी एक या अधिक भाषाओं या हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने का अधिकार देता है।
भाषा का महत्व और नीति समर्थन
- बहुभाषिकता एक जीवनशैली के रूप में: अधिकांश भारतीय दो या अधिक भाषाएँ बोलते हुए बड़े होते हैं।
- बहुभाषिकता अंतरसांस्कृतिक समझ, सामाजिक एकता और विशेष रूप से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती है।
- शिक्षा और सशक्तिकरण: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत कक्षा 5 तक, और जहाँ संभव हो, कक्षा 8 तक मातृभाषा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है।
- JEE, NEET और CUET जैसे प्रतिस्पर्धी परीक्षाएँ अब 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाती हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच विस्तृत हुई है।
- DIKSHA और SWAYAM जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म 130 से अधिक भारतीय भाषाओं में ई-लर्निंग सामग्री प्रदान करते हैं, जिससे डिजिटल अंतर को समाप्त करने में सहायता मिलती है।
- DIKSHA में 33 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण संसाधन उपलब्ध हैं।
- SWAYAM 11 भारतीय भाषाओं में अनुवादित इंजीनियरिंग सामग्री प्रदान करता है।
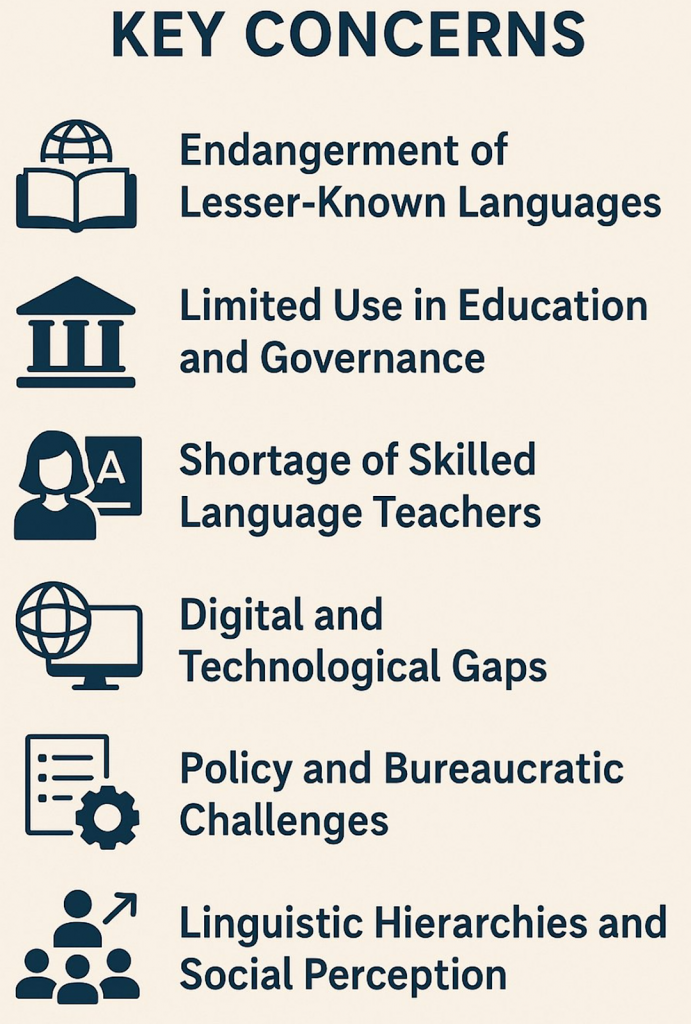
- डिजिटल समावेश और नवाचार: डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, 2017 से भारत में बिकने वाले मोबाइल फ़ोन सभी भारतीय भाषाओं का समर्थन करने चाहिए, जिससे ई-गवर्नेंस और ई-कॉमर्स तक व्यापक पहुंच संभव हुई है।
- भाषिनी जैसी परियोजनाएँ भारतीय भाषाओं के लिए एआई टूल्स विकसित करने का लक्ष्य रखती हैं ताकि तकनीक सभी भाषाई समुदायों की सेवा कर सके।
- लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण: भारत ने विगत पाँच दशकों में 50 भाषाएँ खो दी हैं, और कई जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाएँ अब भी जोखिम में हैं।
- भाषा संवर्धन के लिए समर्पित संस्थान:
- केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL), मैसूरु;
- केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान और CSTT;
- उर्दू और सिंधी भाषाओं के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय परिषदें;
- केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय;
- शास्त्रीय तमिल के केंद्रीय संस्थान (CICT), चेन्नई।
- उद्यम: भारतीय भाषा अनुभाग और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जैसे प्रयास युवाओं में भाषाई सराहना एवं एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।
Previous article
संक्षिप्त समाचार 26-06-2025
Next article
संयुक्त राष्ट्र के 80 वर्ष पूर्ण