पाठ्यक्रम: GS2/ई-शासन
संदर्भ
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने “सुशासन” सम्मेलन में कहा कि भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी शासन में क्रांति लाने में प्रमुख भूमिका निभा रही है।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्या है?
- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी बाह्य अंतरिक्ष में की जाने वाली गतिविधियों को सक्षम करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकियों को नामित करती है:
- जैसे कि पृथ्वी अवलोकन, उपग्रह संचार, उपग्रह नेविगेशन या यहाँ तक कि पृथ्वी की कक्षाओं से परे रोबोट और मानव अंतरिक्ष अन्वेषण।
- सरकारें विकासात्मक गतिविधियों की योजना बनाने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक डेटा और क्षेत्र की जानकारी का उपयोग करती हैं।
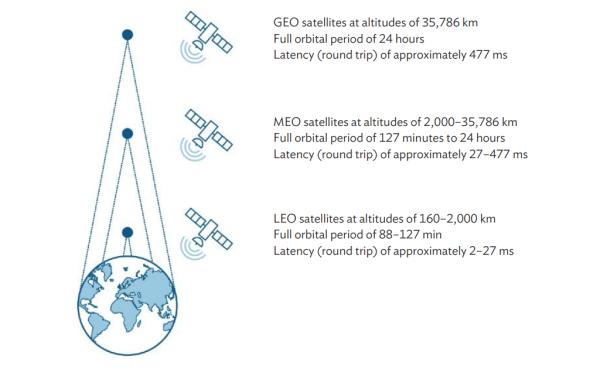
| भविष्य की संभावनाएँ और आर्थिक विकास – विकास: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है, अंतरिक्ष बजट तीन गुना बढ़ गया है और 300 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं। – अंतरिक्ष क्षेत्र का मूल्य 8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 44 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष अभिकर्त्ता बन जाएगा। – महत्त्वपूर्ण मिशन: भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान, गगनयान मिशन के लिए परीक्षण 2025 के अंत तक प्रारंभ हो जाएँगे। भारत का लक्ष्य 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजना और 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। |
शासन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग
- आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया: राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) उपग्रह डेटा प्रदान करता है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान करने, क्षति का मानचित्रण करने और पुनर्वास की योजना बनाने में सहायता करता है।
- भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) आपदा राहत कार्यों के लिए इसका उपयोग करता है।
- कृषि और ग्रामीण विकास: FASAL (अंतरिक्ष, कृषि मौसम विज्ञान और भूमि-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान) फसल की उपज की भविष्यवाणी करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और सिंचाई प्रबंधन को रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके अनुकूलित किया जाता है।
- कुशल भूमि प्रबंधन: “स्वामित्व योजना” जैसी पहल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए उपग्रह मानचित्रण का उपयोग करती है।
- यह पहल भूमि सत्यापन को सरल बनाती है और भूमि स्वामित्व में पारदर्शिता को बढ़ावा देती है।
- पर्यावरण निगरानी: ISRO द्वारा विकसित एक भारतीय वेब-आधारित एप्लिकेशन भुवन विभिन्न पर्यावरणीय और भूमि-उपयोग अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह डेटा प्रदान करता है।
- ओशनसैट शृंखला जैसे उपग्रह समुद्र की सतह के तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय कटाव पर डेटा प्रदान करते हैं।
- सुरक्षा और रक्षा: उपग्रह सीमा निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग में सहायता करते हैं।
- प्रशासनिक दक्षता: सैटेलाइट डेटा ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुँच को सक्षम करके डिजिटल इंडिया पहल के कार्यान्वयन में मदद करता है।
चुनौतियाँ
- उच्च लागत: उपग्रहों का विकास, रखरखाव और प्रक्षेपण महंगा है।
- तकनीकी और बुनियादी ढाँचे की कमी: दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त जमीनी बुनियादी ढाँचे, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी।
- डेटा व्याख्या और सटीकता: अंतरिक्ष-आधारित डेटा को सटीक व्याख्या एवं विश्लेषण की आवश्यकता होती है, और डेटा प्रसंस्करण में त्रुटियों से शासन में गलत निर्णय हो सकते हैं।
- गोपनीयता की चिंताएँ: अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी और निगरानी में वृद्धि नागरिकों के बीच गोपनीयता एवं सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ाती है।
- पर्यावरणीय प्रभाव: अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह प्रक्षेपण में वृद्धि अंतरिक्ष मलबे और पर्यावरण प्रदूषण में योगदान कर सकती है।
आगे की राह
- अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को प्रभावी ढंग से समर्थन देने के लिए आधारभूत बुनियादी ढाँचे, डेटा केंद्रों और संचार प्रणालियों का विकास और उन्नयन करें।
- लागत कम करने, नवाचार को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में सुधार करने के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।
- बेहतर कवरेज के लिए उपग्रहों की संख्या और विविधता बढ़ाएँ, विशेषतः देश के दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
- जलवायु परिवर्तन एवं शहरी नियोजन सहित उभरती शासन चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोगों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करें।
- पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और अंतरिक्ष मलबे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्थायी प्रथाओं को अपनाएँ।
Source: PIB
Previous article
जीन-संपादित केले
Next article
संक्षिप्त समाचार 11-03-2025