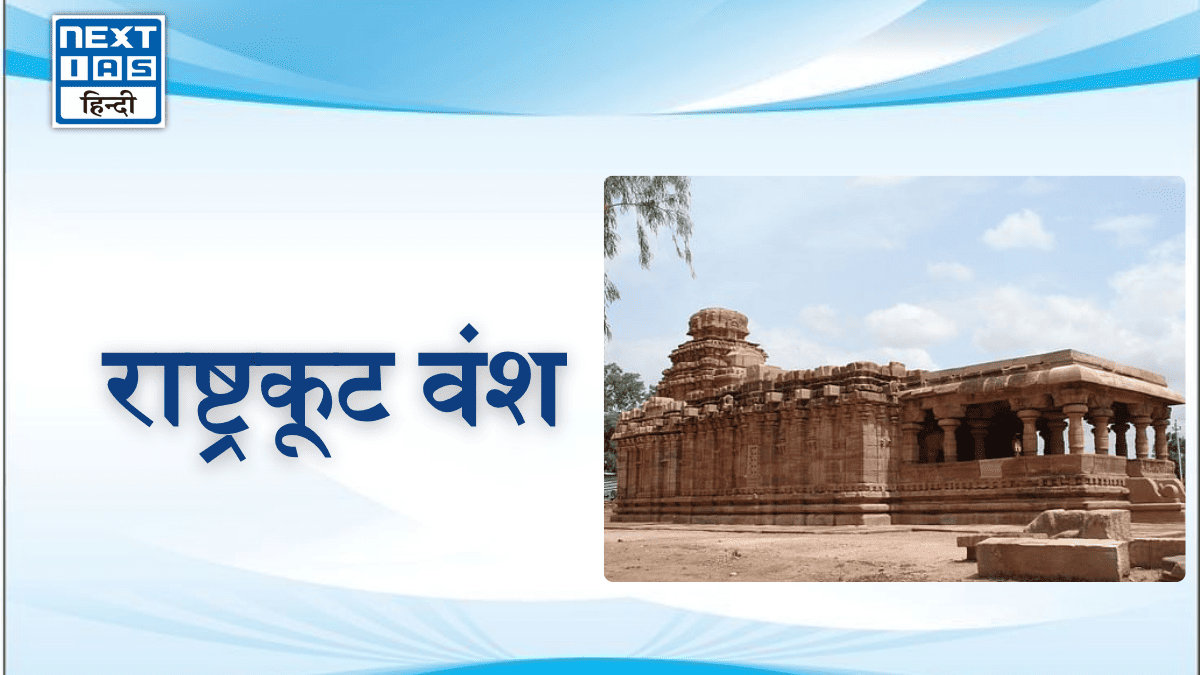मौर्य प्रशासन प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक, मौर्य साम्राज्य के दौरान स्थापित शासन की एक अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल प्रणाली थी। इसका महत्व इसकी उन्नत नौकरशाही संरचना में निहित है, जिसने प्रभावी शासन, सामाजिक कल्याण और साम्राज्य के विस्तार को सुगम बनाया। इस लेख का उद्देश्य मौर्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करना है, जिसमें इसकी संरचना, राजस्व प्रणाली, सैन्य संगठन और लोक कल्याण पहलें आदि शामिल हैं।
मौर्य युग के बारे में
- चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 322 ईसा पूर्व में स्थापित मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था।
- आधुनिक अफ़गानिस्तान से लेकर बंगाल और दक्षिण की ओर दक्कन के पठार तक, साम्राज्य अपने कुशल प्रशासन, सैन्य कौशल और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था।
- अशोक के शासनकाल में, साम्राज्य अपने चरम पर पहुँच गया, बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला और नैतिक शासन पर आधारित नीतियों को लागू किया।
- राजनीतिक एकता, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में मौर्य साम्राज्य के योगदान ने आने वाली भारतीय सभ्यताओं की नींव रखी।
मौर्य प्रशासन
- मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एक विशाल और अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही शासन प्रणाली थी, जिसमें राजा सभी शक्तियों का स्रोत होता था।
- राजा ने कभी भी दिव्य अधिकार (ईश्वरीय सत्ता) का दावा नहीं किया, बल्कि यह एक प्रकार का पारिवारिक अधिनायकवाद था।
- कौटिल्य ने राजा को ‘धर्मप्रवर्तक’ या सामाजिक व्यवस्था का प्रवर्तक बताया।
- केंद्र में सर्वोच्च पदाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था और उन्हें 48000 पण का भुगतान किया जाता था। उनकी संख्या 18 थी।
- कुछ सर्वोच्च पदाधिकारियों में शामिल हैं:
- मंत्री (मुख्य मंत्री),
- पुरोहित (मुख्य पुजारी),
- सेनापति (कमांडर-इन-चीफ), और
- युवराज (युवराज)
मौर्य युग में मंत्रिपरिषद (Council of Ministers)
- मौर्य प्रशासन में, एक मंत्रिपरिषद भी होती थी जो दैनिक प्रशासन में राजा की सहायता करती थी।
- कौटिल्य ने 27 अधीक्षकों (अध्यक्षों) का उल्लेख किया है, जो मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों को विनियमित करने के लिए नियुक्त किये गये थे।
मौर्य युग के अधीक्षकों की सूची
| पण्याध्यक्ष | वाणिज्य |
| संस्थाध्यक्ष | बाजारों की देखरेख, गलत प्रथाओं की जांच |
| पौतवाध्यक्ष | तौल और माप |
| नावाध्यक्ष | राज्य की नौकाएँ |
| शुल्काध्यक्ष | कर/शुल्क |
| सीताध्यक्ष | शाही भूमि |
| अक्षपटलाध्यक्ष | लेखा-जोखा |
| मानाध्यक्ष | माप की व्यवस्था |
| पत्तनाध्यक्ष | बंदरगाह |
| गणिकाध्यक्ष | गणिकाओं की व्यवस्था |
| देवताध्यक्ष | धार्मिक संस्थान |
| लक्षणाध्यक्ष | टकसाल/सिक्का निर्माण |
मौर्य युग में राजनीतिक प्रशासन
मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक प्रशासन निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है:
राजधानी में प्रशासन
- छह समितियाँ, जिनमें से प्रत्येक में पाँच सदस्य होते थे, मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन करती थीं।
- इन समितियों को स्वच्छता, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, वजन और माप का विनियमन और इसी तरह के अन्य कार्य सौंपे गए थे।
प्रांतीय प्रशासन
- राजधानी पाटलिपुत्र को छोड़कर, मौर्य साम्राज्य को चार प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया गया था।
- प्रत्येक प्रांत का शासन एक शासक, राजकुमार या शाही परिवार के सदस्य द्वारा किया जाता था।
| प्रांत का नाम | राजधानी |
|---|---|
| उत्तरपथ (उत्तरी प्रांत) | तक्षशिला |
| अवन्तिराष्ट्र (पश्चिमी प्रांत) | उज्जैन |
| प्राची (पूर्वी व मध्य प्रांत) | पाटलिपुत्र |
| कलिंग (पूर्वी प्रांत) | तोशाली |
| दक्षिणपथ (दक्षिणी प्रांत) | सुवर्णगिरि |
मौर्य युग में जिला प्रशासन
- प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था और उनके तीन मुख्य अधिकारी थे:
- प्रदेशिका: वह जिले के समग्र प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है।
- राजुका: वह राजस्व प्रशासन और बाद में न्यायपालिका के लिए जिम्मेदार था, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रदेशिक के अधीन।
- युक्ता: लेखाकार।
मौर्य युग में उप-जिला और ग्राम प्रशासन
- उप-जिला में 5 से 10 गाँव शामिल होते थे और इनका प्रशासन गोप (लेखाकार) और स्थानिका (कर संग्रहकर्ता) द्वारा किया जाता था।
- गाँवों का प्रशासन एक ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता था जो गोपों और स्थानिकों के लिए जिम्मेदार होता था।
मौर्य युग में नगर प्रशासन
- मेघस्थनीज द्वारा वर्णन के अनुसार, छह बोर्ड, जिनमें से प्रत्येक में पाँच सदस्य होते थे, राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन करते थे।
- इन बोर्डों को औद्योगिक कला, विदेशियों की देखभाल, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, टोल आदि से संबंधित मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
- नागरिका नगर प्रशासन का नेतृत्व करता था और उसे दो अधीनस्थ अधिकारी, स्थानिका और गोप द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
- राजकीय नियंत्रण एक बड़े क्षेत्र तक फैला हुआ था। यह पाटलिपुत्र की रणनीतिक स्थिति के कारण था, जहाँ शाही एजेंट चारों दिशाओं में ऊपर-नीचे नौकायन कर सकते थे।
- राजकीय सड़कें भी अच्छी तरह से बनी हुई थीं और उनका रखरखाव भी किया जाता था। मेगस्थनीज उत्तर-पश्चिमी भारत को पटना से जोड़ने वाली एक सड़क की भी बात करता है।
- अशोक के शिलालेख आवश्यक राजमार्गों पर दिखाई देते हैं। साथ ही अधिक सड़क बस्तियों और रकाब वाले घोड़ों के कारण मध्ययुगीन परिवहन में सुधार हुआ।
मौर्य युग में कर प्रशासन
- मौर्य काल प्राचीन भारत में कराधान प्रणाली में एक मील का पत्थर है।
- कौटिल्य ने किसानों, कारीगरों और व्यापारियों से वसूले जाने वाले कई करों का नाम लिखा है।
- इसके लिए मूल्यांकन, संग्रह और भंडारण के लिए मजबूत और कुशल मशीनरी की आवश्यकता होती होगी। जिस कारण मौर्यों ने संग्रह और भंडारण की तुलना में मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया।
- ‘समहर्ता’ मूल्यांकन का सर्वोच्च अधिकारी था, और ‘सन्निधाता’ राज्य के खजाने और भंडारगृह के मुख्य संरक्षक के रुप में कार्य करता था।
- भूमि राजस्व राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। किसान उपज का एक-चौथाई बाघा और अतिरिक्त बलि/बाली कर के रूप में देते थे।
- पुरालेखीय साक्ष्यों से पता चलता है कि अकाल, सूखे आदि के दौरान स्थानीय लोगों की मदद के लिए अन्न भंडार भी स्थापित किये जाते थे।
मौर्य युग में आर्थिक स्थितियाँ
- कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों ने बहुत प्रगति की। शाही प्रोत्साहनों के कारण, खेती के उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि का उपनिवेशीकरण किया गया।
- बढ़िया और लंबी सड़कों के नेटवर्क और सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के माध्यम से तेज़ संचार के कारण औद्योगिक कला और शिल्प का प्रसार हुआ।
- एक महत्वपूर्ण सामाजिक विकास यह था कि कृषि कार्यों में दासों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। राज्य ने कृषकों और क्षेत्रों (क्षेत्रों/क्षेत्रीय समुदायों) की सहायता से नई भूमि को कृषि में लाया।
- इस नई भूमि से राजस्व में वृद्धि हुई। जिन्हें सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गईं, उनसे उसके लिए शुल्क वसूला गया।
- मौर्यों की प्रमुख मुद्रा छिद्रित मुद्राएं (Punched Marked Coins) थीं, जिन पर मोर, पर्वत, और अर्धचंद्र जैसे चिन्ह अंकित होते थे।
- इनका उपयोग कर वसूली और अधिकारियों को वेतन देने में किया जाता था। इन सिक्कों की एकरूपता के कारण बड़े क्षेत्र में व्यापार विनिमय संभव हो सका
- इस काल की एक अन्य विशेषता थी श्रेणियों (Sherni) और गिल्ड्स (Guilds) का गठन। श्रेणियां कारीगरों और व्यापारियों के संगठन होते थे। व्यापारिक श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थीं।
- ये श्रेणियां बैंक के रूप में भी कार्य करती थीं, जहाँ अमीर लोग अपना धन जमा करते थे।
- शहरी अर्थव्यवस्था में श्रेणियों की महत्ता के कारण उन्हें अधिक स्वायत्तता दी गई थी।
- वे अपने संगठन के संचालन के लिए नियम स्वयं बना सकती थीं। यहाँ तक कि उनके पास न्यायिक अधिकार भी होते थे, अपने सदस्यों के साथ न्याय करने के लिए।
- हालाँकि, यह स्वायत्तता पूर्ण नहीं थी, क्योंकि श्रेणियों को राजा के पास पंजीकरण करवाना आवश्यक होता था, और अंतिम प्रशासनिक नियंत्रण राजा के पास ही रहता था।
- बिक्री के लिए शहर में लाई गई वस्तुओं पर भी टोल लगाया जाता था। राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि पर एकाधिकार प्राप्त था, जिससे स्वाभाविक रूप से शाही खजाने में पैसा आता था।
मौर्य युग में सामाजिक परिस्थितियाँ
- मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को सात जातियों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, सैनिक, पशुपालक, शिल्पकार, मजिस्ट्रेट और सलाहकार।
- उसने जाति को पेशे से भ्रमित कर दिया। फिर भी, उसने गुलामी की अनुपस्थिति को नोट किया, लेकिन भारतीय स्रोत इसका खंडन करते हैं। मौर्यों के दौरान कृषि मजदूरों और घरेलू कामगारों के रूप में दासता मौजूद थी।
- कौटिल्य ने सेना में वैश्यों और शूद्रों की भर्ती की सिफारिश की, लेकिन उनकी वास्तविक भर्ती अत्यधिक संदिग्ध है।
- चार नियमित जातियों के अलावा, वह कम से कम पाँच मिश्रित जातियों का उल्लेख करता है जो आर्य समाज के दायरे से बाहर रहती थीं। शूद्रों को अभी भी तीन वर्णों की सामूहिक संपत्ति माना जाता था।
मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था
- एक विस्तृत गुप्तचर प्रणाली प्रशासनिक तंत्र का समर्थन करती थी। जासूस संन्यासी, भ्रमणशील, भिखारी आदि के वेश में काम करते थे और ये दो प्रकार के होते थे:
- ‘संस्था’ और
- ‘संचारी’।
- संस्था प्रकार के जासूस किसी सार्वजनिक स्थान पर स्थायी रूप से रहकर कार्य करते थे, जबकि संचारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे।
- इस विभाग में तीन प्रकार के अधिकारी होते थे:
- पुलिसानी: जनसंपर्क अधिकारी, जो जनमत एकत्र करता था और उसे राजा को रिपोर्ट करता था।
- प्रतिवेदक: विशेष संवाददाता जिसे किसी भी समय राजा से मिलने की अनुमति होती थी।
- गूढ़पुरुष: गुप्तचर या रहस्य एजेंट।
- चाणक्य ने इस गुप्तचर व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है क्योंकि उन्होंने अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के प्रभाव को रेखांकित किया था।
- चाणक्य ने जासूसों की पात्रता, उनके कार्य करने की विधियाँ और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों पर विस्तृत शिक्षाएं दीं।
मौर्य युग का सैन्य प्रशासन
- मौर्यों के पास एक विशाल सेना थी, और शांतिप्रिय अशोक द्वारा भी इसकी कमी का कोई सबूत नहीं है।
- प्लिनी के अनुसार, चंद्रगुप्त के पास 600,000 पैदल सैनिक, 30000 घुड़सवार और 900 हाथी थे।
- मेगस्थनीज के अनुसार, सेना का प्रशासन छह समितियों द्वारा किया जाता था, जिनमें से प्रत्येक 30 सदस्यों के बोर्ड से बनायी जाती थी।
- ये छह समितियाँ सेना, घुड़सवार सेना, हाथी, रथ, नौसेना और परिवहन थीं।
- अधिकारियों और सैनिकों को नकद भुगतान किया जाता था। मौर्यों के पास एक नौसेना भी थी।
मौर्य कला और वास्तुकला
- चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक समृद्ध मौर्य कला और वास्तुकला भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी अवधि का प्रतीक है।
- इसमें भव्यता और नवीनता की विशेषता है, इसमें स्मारक स्तंभ शामिल हैं, जैसे कि अशोक के स्तंभ, जिनमें पॉलिश किए गए पत्थर की नक्काशी और शिलालेख हैं, और सांची जैसे महान स्तूपों का निर्माण भी शामिल हैं।
- इस युग की कला में बाराबर गुफाओं सहित रॉक-कट गुफाओं का विकास तथा यक्ष और यक्षनियों की आकृतियों वाली महत्वपूर्ण मूर्तिकला का काम भी देखा गया।
- मौर्य काल, विशेष रूप से अशोक के अधीन, बौद्ध रूपांकनों के एकीकरण और कलात्मक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता था, जिसने बाद की भारतीय और एशियाई कला परंपराओं पर गहरा प्रभाव डाला।
मौर्य कला और वास्तुकला पर हमारा विस्तृत लेख पढ़ें।
मौर्य प्रशासन का महत्व
- मौर्य प्रशासन एक अग्रणी प्रणाली थी जिसने प्राचीन भारत में एक कुशल शासन प्रणाली की नींव रखी।
- इसकी केंद्रीकृत संरचना, कुशल नौकरशाही और लोक कल्याण पर जोर उस समय के लिए उल्लेखनीय थे।
- मौर्यों द्वारा स्थापित प्रशासनिक सिद्धांतों और प्रथाओं ने बाद के भारतीय साम्राज्यों को भी प्रभावित किया और शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में उनकी प्रणाली का अध्ययन किया जाता है।
- मौर्य प्रशासन का भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने-बाने पर भी स्थायी प्रभाव पड़ा।
- अपने शिलालेखों और नीतियों के माध्यम से, अशोक ने बौद्ध धर्म, अहिंसा और नैतिक शासन के मूल्यों को बढ़ावा दिया, और एक गहरी विरासत छोड़ी जोकि साम्राज्य की सीमाओं से परे फैली।
- न्याय, कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर मौर्य प्रशासन का ध्यान इसकी समृद्धि और स्थिरता में सहायक बना, जिससे यह भारत के इतिहास के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्यों में से एक बनकर उभरा।
निष्कर्ष
मौर्य प्रशासन एक अत्यंत केंद्रीकृत और कुशल शासन प्रणाली थी, जिसने विशाल भू-भाग वाले साम्राज्य को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद की। इसकी राजस्व व्यवस्था, सैन्य संगठन, न्यायिक प्रणाली, और जनकल्याणकारी पहलों ने इसे शासन का एक ऐसा आदर्श बना दिया, जिसने भविष्य के भारतीय साम्राज्यों के लिए उच्च मानक स्थापित किए। विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य प्रशासन को न्याय, नैतिक शासन, और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है, जिसने प्राचीन भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
मौर्य प्रशासन में प्रमुख अधिकारी कौन-कौन थे?
मौर्य प्रशासन के प्रमुख अधिकारी थे:
– सम्राट
– अमात्य – मंत्रीगण
– महामात्र – उच्च अधिकारी
– सेनापति – सैन्य प्रमुख
– धम्म महामात्र
मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ?
अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों के शासन, प्रशासनिक व्यवस्था का अत्यधिक विस्तार, सैन्य और प्रशासनिक खर्चों के कारण आर्थिक दबाव तथा आंतरिक संघर्षों जैसे कि बार-बार होने वाले विद्रोह और सत्ता संघर्ष के चलते मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इन सभी कारणों ने मिलकर इस शक्तिशाली साम्राज्य के पतन और अंततः इसके विघटन में योगदान दिया।
Read this article in English: Mauryan Administration