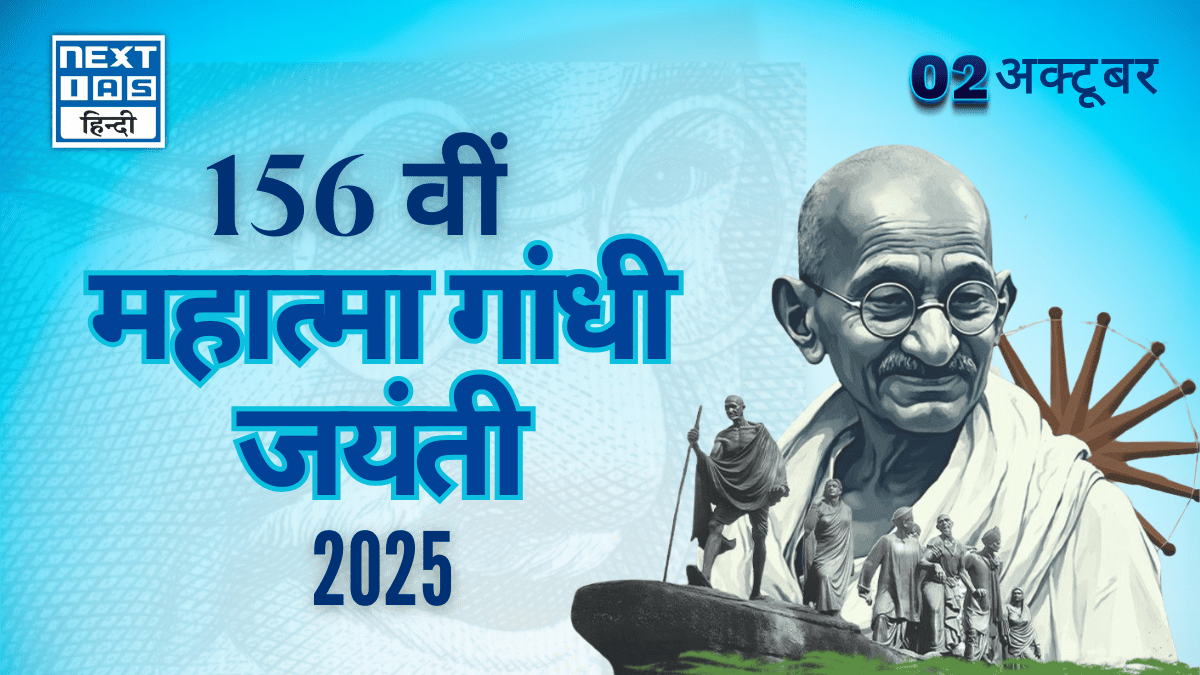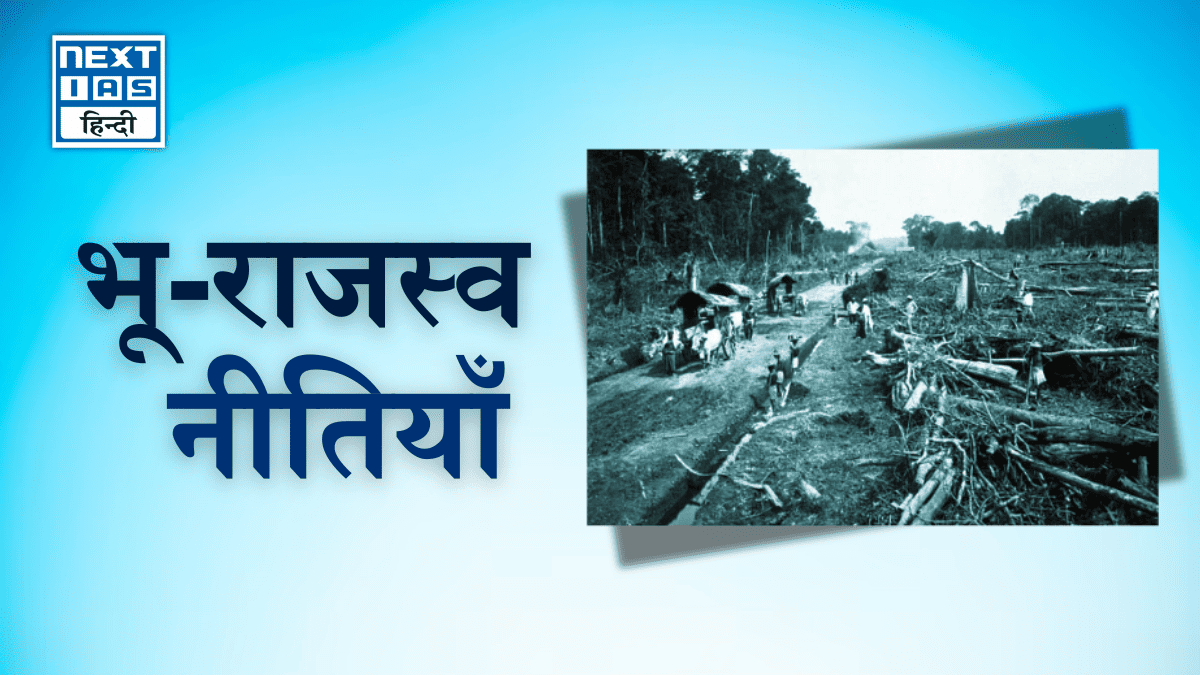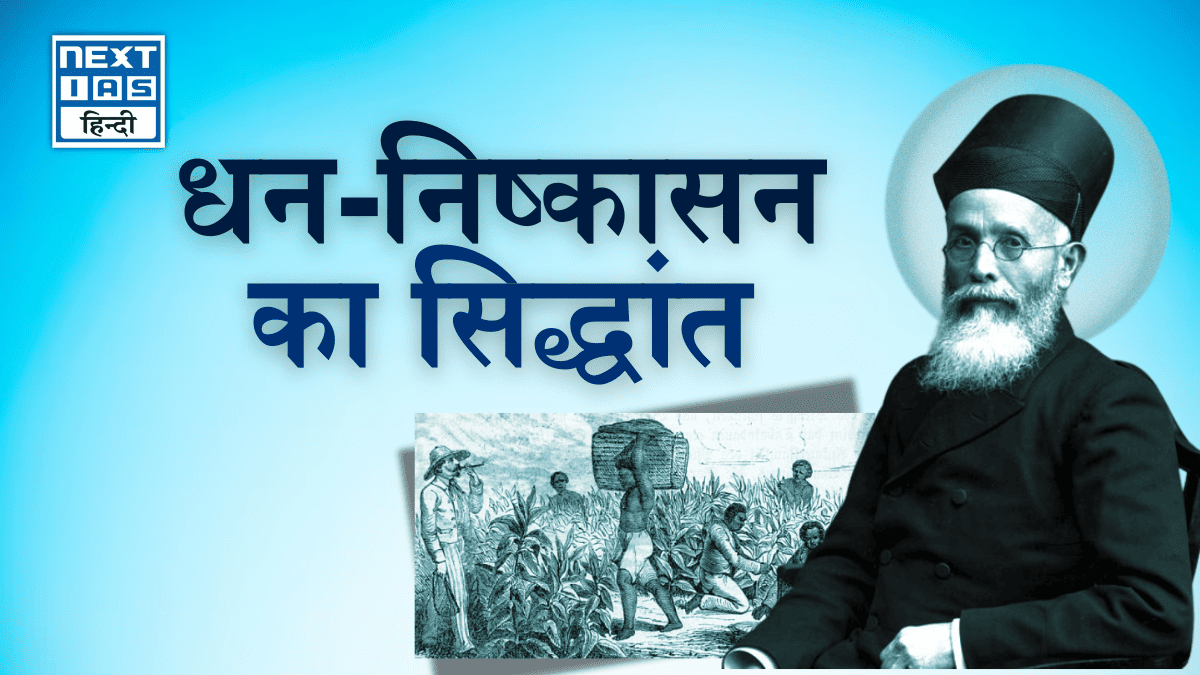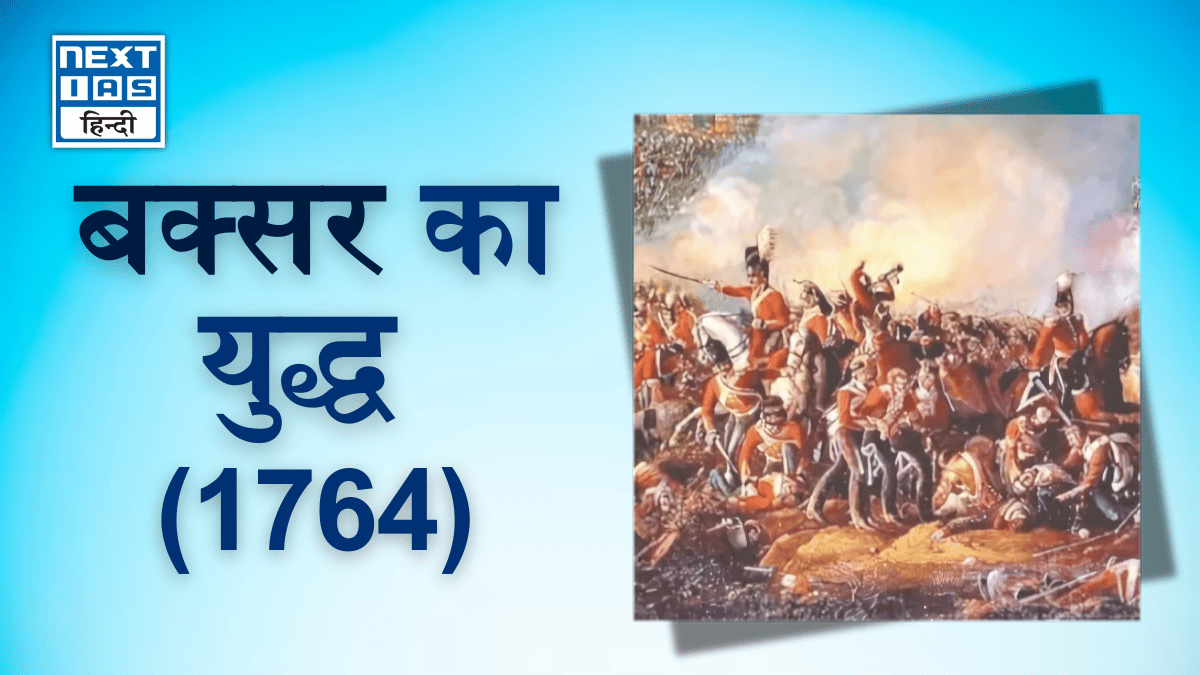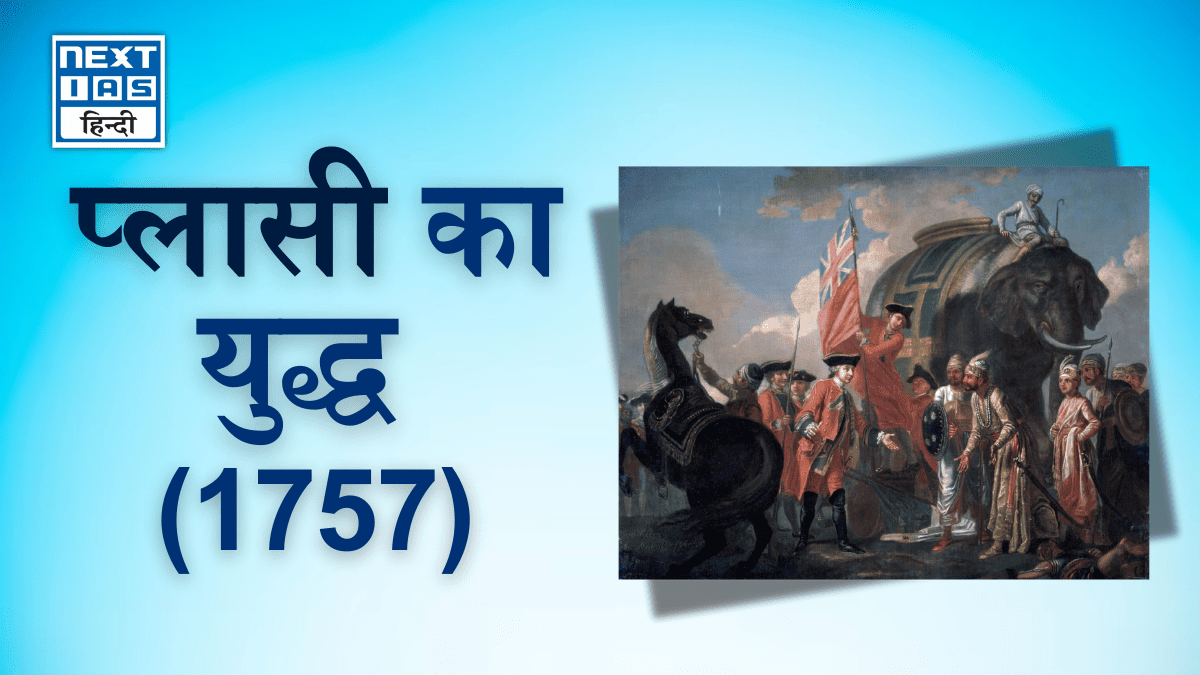मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ई. में की थी। इस वंश ने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी और ऐसे प्रमुख प्रशासनिक व सैन्य ढांचे स्थापित किए जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह लेख मामलुक वंश के प्रमुख शासकों, प्रशासनिक योगदानों, स्थापत्य उपलब्धियों और समग्र विरासत का विस्तार से अध्ययन करने का उद्देश्य रखता है।
मामलुक/गुलाम राजवंश के बारे में
- मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है “स्वामित्व वाला”। इसका उपयोग सैन्य सेवा के लिए आयातित तुर्की दासों को घरेलू श्रम या कारीगरों के रूप में उपयोग किए जाने वाले निचले दासों से अलग करने के लिए किया जाता था।
- दिल्ली सल्तनत के शुरुआती शासक मामलुक थे, जिन्हें गुलाम राजा भी कहा जाता था क्योंकि उनमें से कई या तो गुलाम थे या गुलामों के बेटे थे जो सुल्तान बन गए।
- 1206 ई. में गोरी की मृत्यु के बाद, उसका राजवंश कई भागों में विभाजित हो गया और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया और उसने गुलाम वंश की स्थापना की।
- मुस्लिम मामलुक शासकों ने 1206 ई. से 1290 ई. तक भारत पर शासन किया।
गुलाम वंश का संस्थापक
- गुलाम वंश का संस्थापक, जिसे मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक था।
- वह मूलतः एक गुलाम था, जो ग़ोरी शासक मुहम्मद ग़ोरी के अधीन सेवा करते हुए ऊँचे पद तक पहुँचा। ग़ोरी की विजयों के बाद, ऐबक ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- 1206 ई. में उसने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत हुई।
- उसके शासनकाल की विशेषता कुतुब मीनार के निर्माण सहित महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प उपलब्धियों से थी, और उसे उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है।
- ऐबक के शासनकाल में एकीकरण और विस्तार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसने क्षेत्र में आने वाले अन्य वंशों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
- उसकी विरासत विशेष रूप से एक विशिष्ट इंडो-इस्लामी संस्कृति की स्थापना के लिए उल्लेखनीय है, जो भविष्य में फली-फूली।
मामलुक राजवंश के सभी महत्वपूर्ण शासकों पर निम्नलिखित अनुभाग में विस्तार से चर्चा की गई है।
कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-10 ई.)
- कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे कुशल योद्धाओं में से एक था, जिसने 1206 ई. में मुहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद राजवंश की सेवा की।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खासकर तराइन के दूसरे युद्ध के बाद।
- कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और वह उत्तरी भारत का पहला स्वतंत्र मुस्लिम नेता था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श सुल्तान या लाखों का दाता कहा जाता था।
- कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहादुर और वफ़ादार सिपाही था।
- 1210 में, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान (पोलो) खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण मौत हो गयी।
- कुतुबुद्दीन ऐबक शिक्षा का एक महान संरक्षक था और उसने हसन-उन-निज़ामी और फ़ख़रुद्दीन जैसे लेखकों को संरक्षण प्रदान किया।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार (प्रसिद्ध सूफ़ी संत ख़्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में) का निर्माण शुरू किया, जिसे उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसकी मृत्यु के बाद पूरा किया।
- कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोंपड़ा भी बनवाया।
आराम शाह (1210-1211 ई.)
- कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद, लाहौर के अमीरों और मलिकों ने आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया।
- उसका शासन बहुत ही अल्पकालिक रहा और उसे एक कमजोर एवं अयोग्य शासक माना गया।
- बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया।
शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश (1211-36 ई.)
- इल्तुतमिश मामलुक वंश का दूसरे सबसे प्रमुख शासक था। बगदाद के खलीफा ने उसे “सुल्तान” की उपाधि दी थी।
- अपने कार्यकाल के दौरान, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई महत्वपूर्ण सेनापती- अली मर्दन खिलजी, नासिरुद्दीन कबाचा और ताजुद्दीन यिल्डिज़ स्वतंत्र क्षेत्रों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
- चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों की बढ़ती शक्ति ने सल्तनत की उत्तर-पश्चिमी सीमा को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। इतने बड़े खतरे के बावजूद, उसने कई उपलब्धियों के साथ इस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की।
- उसने चालीस (40) वफादार गुलाम सरदारों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता था, जिसे चालीसा भी कहा जाता था।
- प्रशासन के क्षेत्र में, इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली, सेना और इक्ता में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- उसने ‘इक्ता-दार प्रणाली’ शुरू की जिसमें वेतन के बजाय कुलीनों और उनके अधिकारियों को भूमि प्रदान की जाती थी।
- इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया।
- इल्तुतमिश ने सुल्तान की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय रूप से भर्ती की गई सेना स्थापित करने का प्रयास किया।
- उसने उस काल के दो प्रमुख प्रचलित सिक्कों — चाँदी का टंका और मिश्रधातु का जितल — जारी किए।
- इल्तुतमिश के छब्बीस साल के कार्यकाल को तीन व्यापक चरणों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- पहला चरण (1210-20 ई.): जब वह अपने अधिकार के प्रतिद्वंद्वी दावेदारों से निपटने में व्यस्त रहा।
- दूसरा चरण (1221-27 ई.): इस अवधि के दौरान उसने मंगोल खतरे से निपटा।
- तीसरा चरण (1228-36 ई.): यह एक महत्वपूर्ण अवधि थी जिसके दौरान उसने अपने राजवंश को मजबूत करने के लिए खुद को समर्पित किया।
रुकनुद्दीन फ़िरोज
- इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज को उसकी माँ, शाह तुरकान ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठाया था।
- जब वह राजधानी से बाहर था, तब इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने अवध में उसके विरुद्ध हो रहे विद्रोह को शांत करने के लिए उसे गद्दी से हटा दिया।
रज़िया सुल्तान (1236-40 ई.)
- रजिया सुल्तान सल्तनत और मुगल काल की एकमात्र महिला शासक थीं।
- इल्तुतमिश ने अपने सभी पुत्रों को अयोग्य मानते हुए रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था।
- वह एक कुशल प्रशासक थीं और अपने शासनकाल में पूर्ण कानून और व्यवस्था बनाए रखा।
- रजिया ने मुल्तान, लाहौर और हांसी के विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया।
- उसने एक अबीसीनियाई गुलाम जमाल-उद-दीन याकूत को “घुड़साल प्रमुख” (अखाड़ा) नियुक्त किया।
- तुर्क अमीर और उलेमा, जो अधिकांशतः तुर्क मूल के थे, उसे अपनी शासक मानने को तैयार नहीं थे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा।
- इसी दौरान भटिंडा में एक गंभीर विद्रोह हुआ। भटिंडा के राज्यपाल अल्तुनिया ने रज़िया की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
- रज़िया, याकूत के साथ अल्तुनिया के खिलाफ आगे बढ़ी। हालांकि, अल्तुनिया ने याकूत की हत्या करवा दी और रज़िया को कैद कर लिया।
- बाद में रजिया ने अल्तूनिया से विवाह कर लिया और वे दोनों दिल्ली की ओर कूच कर गए।
- 1240 में, रज़िया एक साजिश का शिकार हो गई और कैथल (हरियाणा) के पास उसकी हत्या कर दी गई।
नासिरुद्दीन महमूद (1246-66 ई.)
- नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का छोटा पुत्र था और उसने 1246 ई. से 1266 ई. तक दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन किया।
- उसे एक दयालु और ईश्वर-भक्त शासक माना जाता था। उसने अपना अधिकांश समय कुरान की आयतें लिखने में बिताया।
- अपने कई पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों के विपरीत, महमूद ने एकपत्नीत्व का सख्ती से पालन किया।
- नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन की पुत्री से विवाह किया और शासन की सारी शक्तियाँ अपने प्रधानमंत्री बलबन को सौंप दीं।
- इब्न बतूता और इस्लामी के अनुसार, बलबन ने नासिरुद्दीन को जहर देकर मार डाला और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया।
ग़ियासुद्दीन बलबन (1266–1287 ई.)
- ग़ियासुद्दीन बलबन, एक तुर्की गुलाम था जिसे उलुग खान के नाम से भी जाना जाता था, ने नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद राजवंश की सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।
- बलबन के कार्यकाल के दौरान दिल्ली और दोआब क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। राजपूत ज़मींदारों ने अवध और गंगा-यमुना दोआब के पूर्वी क्षेत्र में किले स्थापित कर लिए थे।
- बलबन ने सुल्तान की स्थिति को ऊंचा उठाने और निरंकुश शासन को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत की।
- बलबन के शासनकाल को विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण के काल के रूप में जाना जाता है।
- सड़कों पर लुटेरों और डकैतों का आतंक था, इतना कि संचार भी मुश्किल हो गया था।
- इन तत्वों से निपटने के लिए बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। मेवात क्षेत्र में, कई लोगों का निर्दयतापूर्वक पीछा किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
- बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में, राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया गया, जंगलों को काट दिया गया और सड़कों की सुरक्षा के लिए अफगान सैनिकों की कॉलोनियाँ तैनात की गईं। इन कठोर तरीकों से, बलबन ने स्थिति को नियंत्रित किया।
- बलबन के कार्यकाल में कई प्रशासनिक और सैन्य परिवर्तन देखने को मिले :
- बलबन ने सुल्तान की स्थिति को गरिमामय बनाने के लिए सिजदा (साष्टांग दंडवत) और पैबोस (पैर चूमना) की रस्म शुरू की।
- बलबन ने सेना का पुनर्गठन किया और दक्ष गुप्तचर‑तंत्र स्थापित किया।
- बलबन ने चालीसा की शक्ति को तोड़ दिया और ताज की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा।
- बलबन के बढ़ते अधिकार ने कई तुर्की सरदारों को अलग-थलग कर दिया। इसलिए, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा (1253) और बलबन को उसके पद से हटा दिया।
- बलबन की जगह इमादुद्दीन रेहान ने ली, जो एक भारतीय मुसलमान था।
- बलबन का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद ख़ाँ था, जिसकी 1285 ई. में मंगोलों से युद्ध में मृत्यु हो गई।
- अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद, बलबन ने ज़िल-ए-इलाही की भव्य उपाधि धारण की।
- बलबन ने नियामत-ए-खुदिया (ईश्वर का प्रतिनिधि) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
- बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में खुद को ‘खलीफा का सहायक’ लिखवाया।
- मंगोल आक्रमण से रक्षा हेतु साम्राज्य को मज़बूत किलाबंद किया।
- अमीरों को भोग‑विलास त्यागने का आदेश दिया।
- अपनी समृद्धि व शक्ति प्रदर्शित करने के लिए फ़ारसी पर्व नौरोज़ प्रारम्भ किया।
- अनेक मुस्लिम विद्वानों का संरक्षण किया और मध्य एशियाई शरणार्थियों को आसरा दिया।
- बलबन ने सैन्य विभाग (दीवान-ए-अर्ज) को पुनर्गठित किया और देश के विभिन्न भागों में सेना तैनात की।
- बलबन को मुख्य रूप से सरकार और संस्थाओं के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत का मुख्य वास्तुकार माना जाता था।
- 1287 ई. में बलबन की मृत्यु के बाद उसका पौत्र कायक़ुबाद गद्दी पर बैठा।
- इस अवधि के दौरान, सरकारी मामलों में अव्यवस्था फैल गई और कुलीनों ने सत्ता हथियाने के लिए गुट बनाना शुरू कर दिया।
- जलालुद्दीन खिलजी, अरिज-ए-ममालिक (युद्ध मंत्री) ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली और कायक़ुबाद की हत्या कर दी।
- इसके साथ ही 1290 ई. में गुलाम वंश का अंत हुआ और जलालुद्दीन ख़िलजी के नेतृत्व में ख़िलजी वंश की स्थापना हुई।
बलबन का राजत्व सिद्धांत
- बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के व्यापक सिद्धांत को स्पष्ट किया।
- सस्सानीद फारस ने बलबन के राजत्व के सिद्धांत को बहुत प्रभावित किया। उसने दावा किया कि राजा ईश्वर (ज़िल्लाह) की छाया है।
- बलबन का मानना था कि वह केवल सर्वशक्तिमान के प्रति जवाबदेह है और उसके कार्य सार्वजनिक जांच से मुक्त हैं।
सिजदा और पैबोस
- उसने सिजदा (प्रणाम) और पैबोस की शुरुआत की, जिसमें राजा के पैर चूमे जाते थे।
- बलबन पितृसत्तात्मक निरंकुशता में विश्वास करता था। उसका मानना था कि केवल एक निरंकुश ही अपने विषयों से आज्ञाकारिता प्राप्त कर सकता है और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
- बलबन का सबसे बड़ा योगदान केंद्र में एक स्थायी सेना को मजबूत करना और दीवान-ए-अर्ज़ नामक सेना का एक विभाग स्थापित करना था।
- बलबन का मानना था कि राजत्व की महिमा केवल फ़ारसी परंपरा का पालन करके ही संभव है, जिसका उसने अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बहुत सावधानी से पालन किया।
- बलबन ने वंश पर विशेष जोर दिया और स्वयं को काल्पनिक तुर्क वीर अफ़रासियाब का वंशज बताया। उसका राजत्व का सिद्धांत, जो “रक्त और लौह” की नीति से जुड़ा था, उसे बड़े लाभदायक सिद्ध हुआ। इस नीति और दावे के माध्यम से बलबन ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को अत्यंत ऊँचा उठाया।
मामलुक वंश का प्रशासन
- दिल्ली सल्तनत के विस्तार के कारण एक शक्तिशाली और कुशल प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ।
- सुल्तान प्रशासन का मुखिया और एक निश्चित क्षेत्र का स्वतंत्र शासक होता था। शाही घराने की देखभाल के लिए कई अधिकारी होते थे।
- दीवान-ए-विजारत के प्रमुख के रूप में, वज़ीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था।
- विजारत राजस्व संग्रह का आयोजन करता था, व्यय पर नियंत्रण रखता था, खाते बनाये रखता था, वेतन वितरित करता था और सुल्तान के आदेश पर राजस्व असाइनमेंट (इकरा) आवंटित करता था।
- दीवान-ए-अर्ज़, या सैन्य विभाग, का नेतृत्व अरिज-ए-मुमालिक करता था। वह सैन्य मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। वह इक्ता-धारकों द्वारा रखे गए सैनिकों का निरीक्षण करता था।
मामलुक वंश की कला और वास्तुकला
- मामलुक वंश ने अपने शासन के दौरान कई राजसी स्मारक और इमारतें बनवाईं।
- मामलुक या गुलाम वंश द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण इमारतों में शामिल हैं:
- कुतुब परिसर,
- कुतुब मीनार,
- इल्तुतमिश का मकबरा,
- बलबन का मकबरा,
- कुव्वत उल-इस्लाम मस्जिद,
- नासिर-उद-दीन महमूद का मकबरा और
- अढ़ाई दिन का झोपड़ा आदि।
मामलुक राजवंश का महत्व
- मामलुक राजवंश के सुल्तानों ने वास्तुकला में सबसे बड़ा योगदान दिया। भारतीय और इस्लामी परंपराओं के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वास्तुकला की एक इंडो-इस्लामिक शैली विकसित हुई।
- राजनीतिक रूप से, गुलाम राजवंश ने बाद के राजवंशों जैसे खिलजी और तुगलक के लिए एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने की नींव रखी।
निष्कर्ष
मामलुक राजवंश ने शुरुआती दिल्ली सल्तनत को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भारत में भविष्य के मुस्लिम शासकों के लिए मंच तैयार किया। अपनी सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधारों और स्थापत्य उपलब्धियों के माध्यम से, उन्होंने मध्ययुगीन भारत में शासन और सांस्कृतिक विकास के लिए रूपरेखा स्थापित की। उनके योगदान, विशेष रूप से वास्तुकला में, एक स्थायी विरासत छोड़ गए, और उनकी बनाई गई नीतियों को बाद की सल्तनतों जैसे खिलजी और तुगलक वंश ने आगे बढ़ाया और विस्तार दिया। इस तरह ममलूक वंश ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित किया।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था ?
गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था।
मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था?
मामलुक वंश का अंतिम शासक नासिर अल-दीन महमूद था।
दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया?
कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था।
दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन सा था?
दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश मामलुक (गुलाम) राजवंश था।