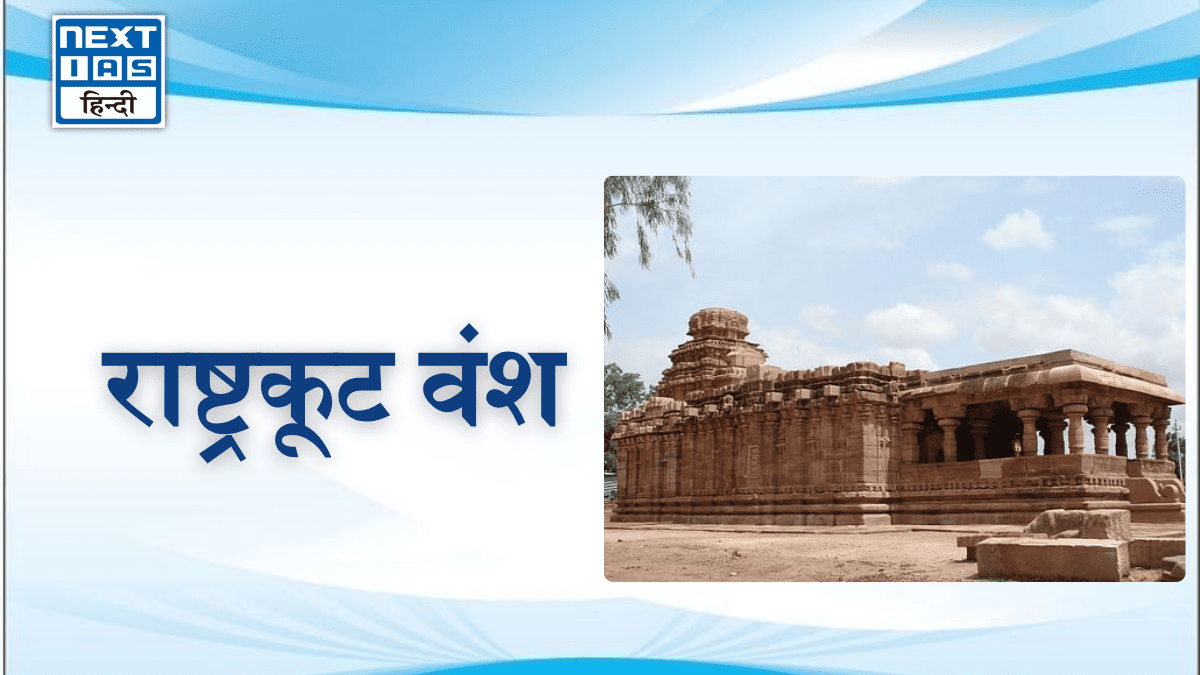प्रारंभिक वैदिक काल (1500–1000 ईसा पूर्व) भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक ऐसा आधारभूत काल था, जिसमें इंडो-आर्यों की उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों, विशेषकर पंजाब और सरस्वती नदी घाटी में बस्तियों का निर्माण हुआ। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसने भारतीय संस्कृति तथा धार्मिक प्रथाओं की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर विकसित होती रहीं। इसका महत्व भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं पर इसके आधारभूत प्रभाव में निहित है, जो पूरे वैदिक काल में विकसित होता रहा। इस लेख का उद्देश्य प्रारंभिक वैदिक काल के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से अध्ययन करना है, जिसमें इसकी सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक प्रथाएँ शामिल हैं।
प्रारंभिक वैदिक काल (ईवीपी) के बारे में
- प्रारंभिक वैदिक काल (1500 – 1000 ईसा पूर्व) वह कालखंड है जब इंडो-आर्यों ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों, मुख्यतः पंजाब और सरस्वती नदी घाटी में बस्ती बसाई।
- इस समय के दौरान, समाज मुख्यतः पशुपालन पर आधारित था, जहाँ कृषि के साथ-साथ पशुओं का पालन एक प्रमुख व्यवसाय था।
- सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ, ऋग्वेद, इसी काल में रचा गया था। यह ग्रंथ लोगों की धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक संरचना और दैनिक जीवन की झलक प्रस्तुत करता है।
- प्रारंभिक वैदिक काल की विशेषता एक सरल, क़बीले-आधारित समाज थी, जहाँ परिवार और क़बीला (जन) सामाजिक संगठन के मुख्य केंद्र थे।
- समाज का संचालन जनजातीय मुखियाओं (राजन) द्वारा किया जाता था, जो न केवल शासन में बल्कि युद्ध में भी अपने लोगों का नेतृत्व करते थे।
- धार्मिक प्रथाएँ विस्तृत अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से अग्नि, इंद्र और वरुण जैसे प्राकृतिक शक्तियों और देवताओं की पूजा पर केंद्रित थीं।
प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक संरचना
प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक संरचना को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- ऋग्वेदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक मशीनरी युद्ध में अपने सफल नेतृत्व के कारण जनजातीय प्रमुख के नेतृत्व में केन्द्र में कार्य करती थी।
- उसे राजन कहा जाता था। राजन एक निरंकुश सम्राट नहीं था, क्योंकि जनजाति की सरकार सभा, समिति, गण और विदथ जैसी जनजातीय परिषदों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार थी।
- दो सबसे महत्वपूर्ण सभाएँ सभा और समिति थीं, जो इतनी प्रभावशाली थीं कि प्रमुख या राजा उनका समर्थन चाहते थे।
- ये कबीले-आधारित सभाएँ विचार-विमर्श, सैन्य और धार्मिक कार्य करती थीं।
- यहाँ तक कि महिलाएँ भी सभा और विदथ में भाग लेती थीं। राजा का पद आम तौर पर वंशानुगत होता था, लेकिन जनजातीय सभा (समिति) द्वारा भी राजा के चुनाव का उल्लेख मिलता है।
प्रारंभिक वैदिक काल के राजाओं की सहायता करने वाले पदाधिकारी
- सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित होता था, जो यज्ञों के माध्यम से जनजाति की शांति में समृद्धि और युद्ध में विजय सुनिश्चित करता था।
- ऋग्वैदिक काल के दो प्रमुख पुरोहित थे वशिष्ठ और विश्वामित्र।
- वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, जबकि विश्वामित्र उदारवादी थे और उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की, जिसका उद्देश्य आर्य जगत का विस्तार करना था। पुरोहितों ने जनजातीय प्रमुखों को प्रेरित किया और उनके कारनामों की प्रशंसा की।
- अगला महत्वपूर्ण पदाधिकारी सेनानी (जनरल) था, जो पड़ोसी जनजातियों के खिलाफ छोटे अभियानों और मवेशियों पर छापे के लिए राजा के अधीन जिम्मेदार था।
- कोई स्थायी सेना नहीं थी; युद्ध के समय राजा मिलिशिया (जनजातीय सशस्त्र बल) का आयोजन करता था। इसमें विभिन्न जनजातीय समूह जैसे व्रत, गण, ग्राम और शर्ध सैन्य कर्तव्यों का निर्वाह करते थे।
- चारागाह भूमि पर अधिकार रखने वाले अधिकारी को व्रजपति कहा जाता था। वह परिवारों के मुखिया (कुलपति) या योद्धा समूहों के प्रमुखों (ग्रामिणी) का नेतृत्व करता था और युद्ध में उन्हें आगे ले जाता था।
- प्रारंभ में ग्रामिणी एक छोटे जनजातीय सैन्य दल का प्रमुख होता था। लेकिन जब ये दल स्थायी रूप से बस गए, तो ग्रामिणी गाँव का मुखिया बन गया और बाद में उसकी पहचान व्रजपति के रूप में होने लगी।
| – विवादों में मध्यस्थ – मध्यमासी – कर संग्राहक – भागदुघ – कोषाध्यक्ष-संगृहीत्री – सारथी- सुता – संदेशवाहक – पालागल – मुनीम-अक्ष्वापा |
प्रारंभिक वैदिक काल की जनजातीय सभा
प्रारंभिक वैदिक काल की जनजातीय सभा को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
विधत
- ऋग्वेदिक काल में विदथ सबसे महत्वपूर्ण सभा थी। इसने धर्मनिरपेक्ष, धार्मिक और सैन्य कार्यों सहित कई उद्देश्यों को पूरा किया।
- सभा की तुलना में, जिसका ऋग्वेद में महिलाओं के संदर्भ में केवल संक्षिप्त उल्लेख मिलता है, विदथ का महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से बार-बार संबंध जोड़ा गया है।
- महिलाएँ पुरुषों के साथ विचार-विमर्श में भाग लेती थीं। विदथ आर्यों की सबसे प्रारंभिक लोक सभा थी, जिसमें आर्थिक, सैन्य, धार्मिक और सामाजिक कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी।
- यह कुलों और जनजातियों के लिए अपने देवताओं की पूजा में शामिल होने के लिए एक सामान्य मंच के रूप में भी कार्य करता था।
सभा
- शब्द सभा का तात्पर्य प्रारंभिक ऋग्वेदिक काल की सभा और बाद के ऋग्वेदिक काल के सभा भवन दोनों से है।
- प्रारंभिक काल में महिलाएँ, जिन्हें सभास्वती कहा गया है, इन सभाओं में भाग लेती थीं। हालाँकि, बाद के वैदिक काल में महिलाओं की भागीदारी समाप्त हो गई।
- ऋग्वेद में सभा को जुए और पासे खेलने का स्थान, साथ ही नृत्य, संगीत, तंत्र-मंत्र और जादू-टोने के मंच के रूप में वर्णित किया गया है।
- सभा का उपयोग पशुपालन से जुड़ी चर्चाओं, साथ ही न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए भी किया जाता था, जिससे यह न्यायिक अधिकारों का अभ्यास करने वाली संस्था बन जाती थी।
समिति
- समिति का उल्लेख ऋग्वेद की बाद की पुस्तकों में मिलता है, जो दर्शाता है कि ऋग्वेदिक काल के अंत में इसने महत्व प्राप्त कर लिया था।
- समिति एक लोक सभा थी, जहाँ जनजाति के सदस्य जनजातीय मामलों को संभालने के लिए एकत्रित होते थे।
- इसने दार्शनिक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा धार्मिक समारोहों और प्रार्थनाओं में भाग लिया। अभिलेखों से पता चलता है कि राजा का चुनाव और पुनः चुनाव समिति द्वारा किया जाता था।
सभा और समिति की तुलना
- शुरूआत में, सभा और समिति के बीच कोई अंतर नहीं था; दोनों को प्रजापति की बेटियाँ कहा जाता था तथा ये प्रमुखों के नेतृत्व में चलती-फिरती इकाइयों के रूप में कार्य करती थीं, जो अपनी सेनाओं के साथ यात्रा करते थे।
- मुख्य अंतर यह था कि सभा न्यायिक कार्य करती थी, जो समिति को नहीं दी जाने वाली भूमिका थी।
- समय के साथ, सभा एक छोटी कुलीन संस्था के रूप में विकसित हुई, जबकि समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया।
प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था की प्रकृति
प्रारंभिक वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- मुख्य रूप से ग्रामीण- वैदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण थी, जिसमें सीमित खाद्य उत्पादन और शहरी आबादी का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे।
- मुख्य रूप से पशुपालन अर्थव्यवस्था- ऋग्वेद में गाय और बैल के कई संदर्भ हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ऋग्वेदिक आर्य मुख्य रूप से पशुपालक थे। चरवाहे और चरागाह जैसे शब्दों से पता चलता है कि वे खानाबदोश थे जो अपने जानवरों को चराने के लिए इधर-उधर घूमते थे।
- कृषि- आर्यों के लिए कृषि भी एक प्राथमिक व्यवसाय था। उन्हें बुवाई, कटाई और थ्रेसिंग सहित कृषि का बेहतर ज्ञान था और वे विभिन्न मौसमों से अवगत थे। क्षेत्र में आर्यों से पूर्व भी रहने वाले लोग कृषि के बारे में जानते थे, लेकिन वह मुख्य रूप से चारा उत्पादन के लिए करते थे।
- सिंचाई के कृत्रिम साधन- नहरों और कुओं के संदर्भ सिंचाई के कृत्रिम साधनों का उपयोग करने का संकेत देते हैं।
- पशुओं का पालन- गाय को बहुत महत्व दिया जाता था और उसे ‘सभी अच्छे गुणों का योग’ कहा जाता था। ऋग्वेदिक आर्य गायों और बैलों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानते थे।
- गाय मूल्य का एक माप थी, जिसे “गोधन” या गाय की संपत्ति कहा जाता था।
- गाय का दूध मुख्य भोजन था, और इससे बलि के लिए घी बनाया जाता था।
प्रमुख व्यवसाय और भूमि का स्वामित्व
आरंभिक वैदिक काल के प्रमुख व्यवसायों को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- कुछ विद्वानों के अनुसार, जब ऋग्वेदिक आर्यों ने पहली बार भारत में प्रवेश किया, तो उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन वाली थी।
- पशुपालन, विशेष रूप से गौपालन, उनका मुख्य व्यवसाय था। धीरे-धीरे, उन्होंने कृषि को अपनाया, जो उनके प्रमुख व्यवसायों में से एक बन गया।
- आखिरकार, कृषि और पशुपालन ऋग्वेदिक आर्यों के दो प्रमुख व्यवसाय बन गए। धान (ब्रीही) और जौ जैसे खाद्यान्न उगाए जाते थे।
उद्योग
आरंभिक वैदिक काल के उद्योग को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- कपास और ऊन की बुनाई ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य उद्योग था। इस उद्योग में पुरुष और महिला दोनों लगे हुए थे।
- बढ़ई रथ, हल, गाड़ियाँ और घर बनाते थे। बढ़ईगीरी एक आकर्षक पेशा था।
- आर्य तकनीकी रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित थे। लोहार हथियार और घरेलू उपकरण बनाते थे, और सुनार आभूषण बनाते थे।
- उनके कांस्य कारीगर अत्यधिक कुशल थे, जो हड़प्पा संस्कृति के कारीगरों से कहीं बेहतर औजार और हथियार बनाते थे।
- कांस्य कारीगर, बढ़ई और रथ बनाने वालों का ऋग्वेद में अक्सर बहुत सम्मान के साथ उल्लेख किया गया है।
व्यापार और वाणिज्य
प्रारंभिक वैदिक काल के व्यापार और वाणिज्य को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- आरंभिक वैदिक समाज के ऋग्वेदिक लोग एक ही जनजाति के सदस्यों और अन्य जनजातियों के साथ व्यापार करते थे।
- कभी-कभी, व्यापारी व्यापार में अधिक लाभ के लिए दूर-दूर की यात्राएँ करते थे।
- जंगलों की कटाई और पूर्वी भारत में आर्य बस्तियों के विस्तार ने व्यापार की मात्रा में वृद्धि की।
- यमुना और सिंधु की सहायक नदियों के किनारे आर्य गाँवों से भरे हुए थे। उनके बीच व्यापार संभवतः नदी मार्ग से होता था।
- भूमि मार्ग से भी व्यापार किया जाता था।
परिवहन और व्यापार का माध्यम
आरंभिक वैदिक काल के व्यापार के माध्यम को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- भूमि मार्ग से परिवहन के मुख्य साधन रथ (रथ) तथा घोड़े और बैलों द्वारा खींचे जाने वाले वैगन थे, जबकि नदी मार्ग के लिए नावों का उपयोग किया जाता था।
- व्यापार का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मवेशी एक प्रकार की मुद्रा थे, और मवेशियों के सिर में मूल्य गिना जाता था, लेकिन इस समय उन्हें पवित्र नहीं माना जाता था। भोजन के लिए बैल और गाय दोनों का वध किया जाता था।
- घोड़ा गाय के समान ही अत्यंत महत्वपूर्ण था। यद्यपि घुड़सवारी का उल्लेख मिलता है, लेकिन घोड़े को मुख्य रूप से रथ की प्रमुख शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। यह रथ हल्का होता था, जिसमें दो तिल्लेदार पहिए होते थे। इसे दो समानांतर जुते हुए घोड़े खींचते थे और इस पर दो योद्धा सवार होते थे।
- धीरे-धीरे, “निष्क” नामक सोने के टुकड़ों का आदान-प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाने लगा।
- वाणिज्य का प्रबंधन आम तौर पर पणि नामक लोगों के एक वर्ग द्वारा किया जाता था, जो संभवतः गैर-आर्यन थे। आर्य उन्हें बहुत चतुर मानते थे।
विदेशी व्यापार
प्रारंभिक वैदिक काल के विदेशी व्यापार को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- हमें नहीं पता कि आर्यों का पश्चिम एशियाई देशों के साथ विदेशी व्यापार था या नहीं। हड़प्पावासियों का पश्चिम एशिया के साथ व्यापक व्यापार था, लेकिन यह निश्चित नहीं है कि आर्य इसे जारी रख पाए या नहीं।
- चूँकि ऋग्वेदिक युग में आर्य सभ्यता हड़प्पावासियों की तुलना में कम औद्योगिक और कम शहरी थी, इसलिए यह माना जा सकता है कि आर्यों का व्यापार स्थानीय था।
- कुछ विद्वानों का मानना है कि ऋग्वेद एक विशाल व्यापार का उल्लेख करता है जो केवल बाहरी व्यापार ही हो सकता है।
प्रारंभिक वैदिक काल का सामाजिक जीवन
पारिवारिक जीवन
- आर्यों का पारिवारिक जीवन बहुत सरल था, परन्तु परिवार के सबसे बड़े सदस्य के नेतृत्व में अच्छी तरह से व्यवस्थित था।
- परिवार प्रणाली पितृसत्तात्मक समाज पर आधारित थी।
- परिवार या कुल का शासन पुरुष सदस्य करते थे। परिवार के मुखिया या कुल के प्रमुख को कुलप कहा जाता था (संस्कृत शब्द ‘पा’ से व्युत्पन्न, जिसका अर्थ है ‘सुरक्षा करना’)।
- उन्हें परिवार की भलाई, जीवन और संपत्ति की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी।
- आम तौर पर, परिवार संयुक्त जिम्मेदारी पर आधारित था, जहाँ महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त थी।
- परिवार के मुखिया सामान्यतः पारिवारिक प्रार्थना का नेतृत्व करते थे, और महिलाएं इसमें सम्मिलित हो सकती थीं और कभी-कभी अग्रणी भूमिका भी निभा सकती थीं।
महिलाओं की स्थिति
प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति निम्नलिखित प्रकार देखी जा सकती है:
- ऋग्वेदिक परिवार पितृवंश पर आधारित थे और एक पुत्र का जन्म हमेशा अपेक्षित मन जाता था। पुत्र रहित जोड़े को गरीबी के समान देखा जाता था। पुत्रों को गोद लेने का भी स्वागत किया जाता था।
- हालांकि, जब कोई पुत्री जन्म लेती थी तो उसकी उपेक्षा नहीं की जाती थी और उसको शिक्षा से भी वंचित नहीं किया जाता था।
- ऋग्वेदिक समाज में घोष, विश्ववारा, और अपाला जैसी महिला विदुषियाँ प्रसिद्ध थीं, और कुछ वैदिक सूक्त भी उनकी रचना माने जाते हैं।
- महिलाएं सभाओं में भाग ले सकती थीं और अपने पतियों के साथ यज्ञ अर्पित कर सकती थीं।
- किसी लड़की को पिता के अंतिम संस्कार करने का अधिकार नहीं था। पत्नी धार्मिक अनुष्ठानों में अपने पति के साथ भाग ले सकती थीं और उन्हें गृहिणी का शीरषक प्राप्त था, जो पति, बच्चों, बुजुर्ग ससुर तथा गृहस्थ सेवकों की देखरेख करती थीं।
- यहां पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था।
- त्योहारों में महिलाओं को स्वतंत्र रूप से भाग लेने की आजादी थी।
- लड़कियों का विवाह आम तौर पर युवावस्था (किशोरावस्था) के बाद किया जाता था, परन्तु बाल विवाह की प्रथा ज्ञात नहीं है।
- ऋग्वेद में विवाहयोग्य आयु लगभग 16 से 17 वर्ष मानी जाती प्रतीत होती है। दुल्हन और दूल्हे दोनों को स्वतंत्र पसंद की अनुमति थी।
- प्रेम विवाह अप्रचलित नहीं था। यदि कोई दहेज प्रत्याशित नहीं था, तो अनिच्छुक दामाद को दहेज का भुगतान करना पड़ता था।
- प्रेम विवाह कोई नई बात नहीं थी। अवांछित दामाद को वधू-मूल्य देना पड़ता था। दहेज और वधू-मूल्य दोनों को मान्यता दी गई थी। शारीरिक रूप से विकलांग लड़कियों को विवाह के दौरान उचित दहेज दिया जाता था।
- बहुविवाह का प्रचलन था, लेकिन बहुपतित्व के संकेत भी मिलते हैं। हालाँकि, प्रारंभिक वैदिक काल में एकपत्नीत्व सामान्य नियम था।
- विधवाओं का पुनर्विवाह अनुमत था।
- भाई की विधवा से विवाह की प्रथा प्रचलित थी।
- ऋग्वेदिक कानून के अनुसार महिलाओं को स्वतंत्र नहीं माना जाता था और उन्हें अपने पुरुष संबंधियों के संरक्षण में रहना पड़ता था।
सामाजिक विभाजन
प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक विभाजनों को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है:
- ऋग्वेद में लगभग 1500-1000 ईसा पूर्व उत्तर-पश्चिमी भारत में लोगों की शारीरिक रूपरेखा की कुछ झलक मिलती है।
- ‘वर्ण’ शब्द का अर्थ रंग था, और ऐसा प्रतीत होता है कि आर्य भाषी लोग उज्ज्वल वर्ण के थे, जबकि स्वदेशी निवासी (दास्य) गहरे वर्ण के थे।
- सामाजिक विभाजनों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान स्वदेशी निवासियों पर आर्यों द्वारा किए गए विजय ने दिया।
- दास और दास्य, जिन्हें आर्यों ने जीत लिया था, उन्हें दास और क्षुद्र के रूप में देखा जाता था।
- ऋग्वेद में आर्यवर्ण और दासवर्ण का उल्लेख मिलता है।
- जनजातीय मुखिया और पुरोहित लूट का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते थे, जिससे स्वाभाविक रूप से अपने कुटुंबियों की लागत पर उनकी स्थिति मजबूत होती जाती थी और इससे जनजाति में सामाजिक असमानताएँ उत्पन्न हो जाती थीं।
प्रारंभिक वैदिक काल का समाज
समाज की संरचना
प्रारंभिक वैदिक काल के समाज की संरचना इस प्रकार थी:
- ऋग्वैदिक युग के दौरान समाज की नींव परिवार था; शक्ति की मूल इकाई एक पितृसत्तात्मक परिवार (कुल) में निहित थी।
- ऐसे परिवारों का एक समूह ग्राम कहलाता था, जिसका नियंत्रण ग्रामिनी द्वारा किया जाता था।
- ग्रामों के समूह को वंश (विश) कहा जाता था और कई वंश मिलकर एक जन समुदाय बनाते थे।
- विश संभवतः युद्ध के लिए बने छोटे-छोटे ग्राम या जनजातीय इकाइयों में विभाजित था।
समाज की प्रकृति
आरंभिक वैदिक काल के समाज की प्रकृति को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- पितृसत्तात्मक समाज- परिवार पूरी तरह से पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक था। पत्नी को सम्मानित स्थान प्राप्त था, फिर भी वह अपने पति के अधीन मानी जाती थी।
- विवाह आमतौर पर एकपत्नीत्व और अविभाज्य था, जिसमें तलाक का कोई संदर्भ नहीं मिलता है। एक बेटे का जन्म अत्यधिक वांछित था, और लोग युद्ध में लड़ने के लिए बहादुर बेटों के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे।
- समतावादी समाज- ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था संगठित रूप में विद्यमान नहीं थी।
- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जैसे वर्गों का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं था। कोई भी व्यक्ति किसी भी पेशे को अपना सकता था, क्योंकि व्यवसाय का कोई स्थायी जातिगत संबंध नहीं था।
- ग्रामीण सभ्यता – आरंभिक ऋग्वेदिक समाज के लोग मुख्य रूप से गाँवों में रहते थे। घर लकड़ी या ईख के भूसे से बने होते थे और उनमें कई अपार्टमेंट होते थे।
- कभी-कभी आक्रमण के समय शरण लेने के लिए किलाबंद स्थानों को “पुर” कहा जाता था। “पुर” का अर्थ आवश्यक रूप से नगर या शहर नहीं था, क्योंकि इस काल में नगरों और शहरों की संख्या बहुत कम थी।
- जीवन के चार आश्रम – ऋग्वैदिक युग के उत्तरार्ध में चार आश्रमों का आदर्श विकसित हुआ।
- उच्च वर्गों के बालक ब्रह्मचर्य के रूप में आचार्यों के घर पर रहकर व्याकरण, छंदशास्त्र, काव्य और वेदों का अध्ययन करते थे।
- इसके बाद वे गृहस्थ (गृहस्वामी), फिर वानप्रस्थ (वनवासी), और अंततः संन्यास (त्यागी) के चरण में प्रवेश करते थे।
- मनोरंजन के तरीके- पुरुष और महिलाएँ दोनों ही नृत्य और गायन का आनंद लेते थे। घुड़दौड़ और जुआ पुरुषों के विशेष मनोरंजन के साधन थे।
- आर्यजन संगीत प्रेमी थे; वे बांसुरी और वीणा बजाते थे, जिनमें झांझ और नगाड़ों की संगत होती थी। वे सप्तस्वरी (सात स्वरों) का प्रयोग करते थे। रथ दौड़ भी एक अत्यंत लोकप्रिय खेल थी।
- वस्त्र- ऋग्वैदिक काल के लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, और कभी-कभी मृगचर्म (हिरण की खाल) भी प्रयोग में लाते थे।
- पुरुष सामान्यतः एक नीचे का वस्त्र (वास) और एक ऊपर का वस्त्र (अधिवास) पहनते थे। महिलाएँ इसके अतिरिक्त एक अंतःवस्त्र पहनती थीं, जिसे “नीवि” कहा जाता था।
- आभूषण- ऋग्वेदिक महिलाएँ कई तरह के सोने के आभूषण पहनती थीं, जिनमें कभी-कभी कीमती पत्थर जड़े होते थे।
- महिलाएँ लंबे बाल रखती थीं, जिन्हें कंघी करके, तेल लगाकर और लटों में बाँधकर रखा जाता था। अमीर लोग रंगीन और कढ़ाई वाले कपड़े पहनते थे। पुरुष और महिलाएँ दोनों ही आभूषण पहनते थे।
- खान-पान की आदतें- दैनिक आहार में जौ, चावल, सेम, सब्जियाँ, दूध, दुग्ध उत्पाद और केक (पकवान) शामिल थे।
- वे मांसाहारी भोजन भी करते थे, जिनमें मछली, पक्षी, बकरियाँ, बैल और घोड़े तक शामिल थे। वे नशीले पेय पीते थे जिन्हें “सुरा” और “सोम” कहा जाता था (ये पौधों के रस से तैयार किए जाते थे)।
- सोम का प्रयोग यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों में होता था और इसे पवित्र माना जाता था, जबकि सुरा एक सांसारिक और अधिक तीव्र नशा देने वाला पेय था, जिसे पुरोहित कवियों द्वारा नापसंद किया गया था।
- विशेष यज्ञों के लिए ब्राह्मण की विशेषज्ञ देखरेख आवश्यक होती थी, परंतु सामान्य अनुष्ठान और समारोहों का संचालन परिवार का मुखिया स्वयं करता था।
- विवाह की संस्था- वैदिक काल में विवाह संस्था का विकास हो चुका था, यद्यपि कुछ प्राचीन परंपराओं के चिह्न अभी भी प्रचलित थे। यद्यपि दुर्लभ, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुपतित्व (एक स्त्री के कई पति) के संकेत भी मिलते हैं।
- मातृवंशीय परंपराओं के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे ममतयेय (ममता का पुत्र) जैसे उदाहरणों में, जहाँ पुत्र माता के नाम से पहचाना जाता है।
प्रारंभिक वैदिक काल का धार्मिक जीवन
प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक जीवन को निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
- प्रारंभिक वैदिक धर्म को हेनोथीज़्म (Henotheism) या कथेनोथीज़्म (Kathenotheism) के नाम से जाना जाता है — यह ऐसी मान्यता थी जिसमें एक समय में किसी एक देवता को ही सर्वोच्च माना जाता था। इस काल के धर्म को प्रकृति की पूजा के रूप में भी वर्णित किया गया है।
- एक अन्य प्रमुख विशेषता एकेश्वरवाद (Monotheism) और यहाँ तक कि अद्वैतवाद (Monism) की ओर प्रवृत्ति थी।
- देवताओं के प्रतीक के रूप में भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना पूरी तरह से अज्ञात नहीं था। मृत्यु के बाद जीवन के संबंध में, ऋग्वेदिक भजनों में कोई सुसंगत सिद्धांत नहीं है।
- प्राकृतिक शक्तियों को मानव रूप में कल्पित किया गया था और उन्हें जीवित प्राणी समझा जाता था। आर्य लोग प्रकृति का अत्यंत सम्मान करते थे, और जहाँ कहीं उन्हें सौंदर्य या शक्ति का अनुभव होता, वे उस प्राकृतिक तत्व के प्रति श्रद्धा से सिर झुका देते और उससे कृपा की याचना करते।
- अग्नि और इन्द्र जैसे देवताओं को पूरे जन समुदाय (कबीला) द्वारा किए गए यज्ञों में आमंत्रित किया जाता था।
- देवताओं को सब्जियाँ, जौ आदि अर्पित किए जाते थे। लोग मुख्यतः संतान (प्रजा), पशु (पशु), अन्न, धन, स्वास्थ्य आदि की कामना करते थे।
- ऋग्वेद, जो मुख्य रूप से एक धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक विश्वासों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है।
- उस समय का धर्म सरल और सभी औपचारिकताओं से मुक्त था। एकमात्र सामूहिक प्रार्थना यज्ञ थी।
प्रारंभिक वैदिक काल का महत्व
प्रारंभिक वैदिक काल का महत्व निम्न रूप में देखा जा सकता है:
- देश का नाम भरत नामक कुल के नाम पर पड़ा।
- आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व: यह वही काल था जब भारत ने मानव संस्कृति को अपनी सबसे बहुमूल्य योगदानों में से एक वैदिक साहित्य प्रस्तुत किया।
- सांस्कृतिक आपसी संपर्क: इस काल में भाषाओं का आदान-प्रदान हुआ, जिसमें संस्कृत, ग्रीक और लैटिन जैसी भाषाओं में कई समान शब्द पाए गए, जो सांस्कृतिक मेल-जोल को दर्शाते हैं।
- समाज में एक मजबूत पारिवारिक व्यवस्था थी और सामाजिक विभाजन और असमानताएँ कम थीं।
- महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और इस अवधि के दौरान कई महिला विद्वान उभरीं।
प्रारंभिक वैदिक काल की सीमाएँ
प्रारंभिक वैदिक काल की सीमाएँ निम्नलिखित थीं:
- इस काल में विभिन्न भेदभावों की शुरुआत हुई, जो बाद के वैदिक काल में महिलाओं की नीची स्थिति, जातिवाद, पितृसत्तात्मक मानसिकता, अनगिनत अनुष्ठान, मूर्तिपूजा और वर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आए।
- लगातार आपसी और अंतर-जनजातीय युद्धों के कारण लोगों और भौतिक वस्तुओं की हानि हुई, जो अन्यथा समाज के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती थी।
- पुजारियों की स्थिति मजबूत हुई, जबकि निचली जातियों की स्थिति खराब हुई।
- रक्त शुद्धता की अवधारणा के साथ एक वंशानुगत और व्यवसाय-आधारित जाति और वर्ग व्यवस्था मजबूत हुई।
- दासता के कुछ उदाहरण मिले, लेकिन ये केवल अस्पष्ट (nebulous) अवस्था में थे और समाज में इसके व्यापक रूप से अस्तित्व का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं था।
प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर
प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बीच अंतर निम्न प्रकार देखा जा सकता है:
| पक्ष (Aspect) | प्रारंभिक वैदिक काल (Early Vedic Period) | उत्तर वैदिक काल (Later Vedic Period) |
| ग्रंथ | मुख्यतः ऋग्वेद | यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद |
| समाज | पशुपालक, अर्ध-घुमंतू, पशुपालन पर केंद्रित | स्थायी, कृषिक, वर्ण व्यवस्था का विकास |
| राजनीतिक संगठन | जनजातीय संरचना, मुखिया (राजा) | बड़े राज्य, गणराज्य (महाजनपद), अधिक केंद्रीकृत सत्ता |
| धार्मिक प्रथाएं | अग्नि यज्ञ, प्राकृतिक देवताओं की पूजा | जटिल अनुष्ठान और दार्शनिक अवधारणाएँ (ब्रह्म, आत्मा) |
| भाषा | वैदिक संस्कृत (कम जटिल) | शास्त्रीय संस्कृत (अधिक परिष्कृत) |
निष्कर्ष
प्रारंभिक वैदिक काल प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को आकार देने वाला एक महत्वपूर्ण काल था। यह काल मजबूत पारिवारिक व्यवस्था, तुलनात्मक सामाजिक समानता और वैदिक साहित्य में महत्वपूर्ण योगदानों से चिह्नित रहा। हालांकि, इसी काल ने आगे चलकर सामाजिक वर्गीकरण और जटिलताओं की नींव भी रखी। इस युग की विरासत में प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान, विकसित होती धार्मिक प्रथाएँ और प्रारंभिक सामाजिक संरचनाएँ शामिल हैं, जिन्होंने आगे के ऐतिहासिक विकास को प्रभावित किया। प्रारंभिक वैदिक काल को समझना उन सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की उत्पत्ति को जानने में मदद करता है जो आज भी भारत में गूंजती हैं।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रारंभिक वैदिक काल क्या है?
प्रारंभिक वैदिक काल (लगभग 1500–1000 ईसा पूर्व) वह समय है जब ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो ऋचाओं और अनुष्ठानों का एक संकलन है।