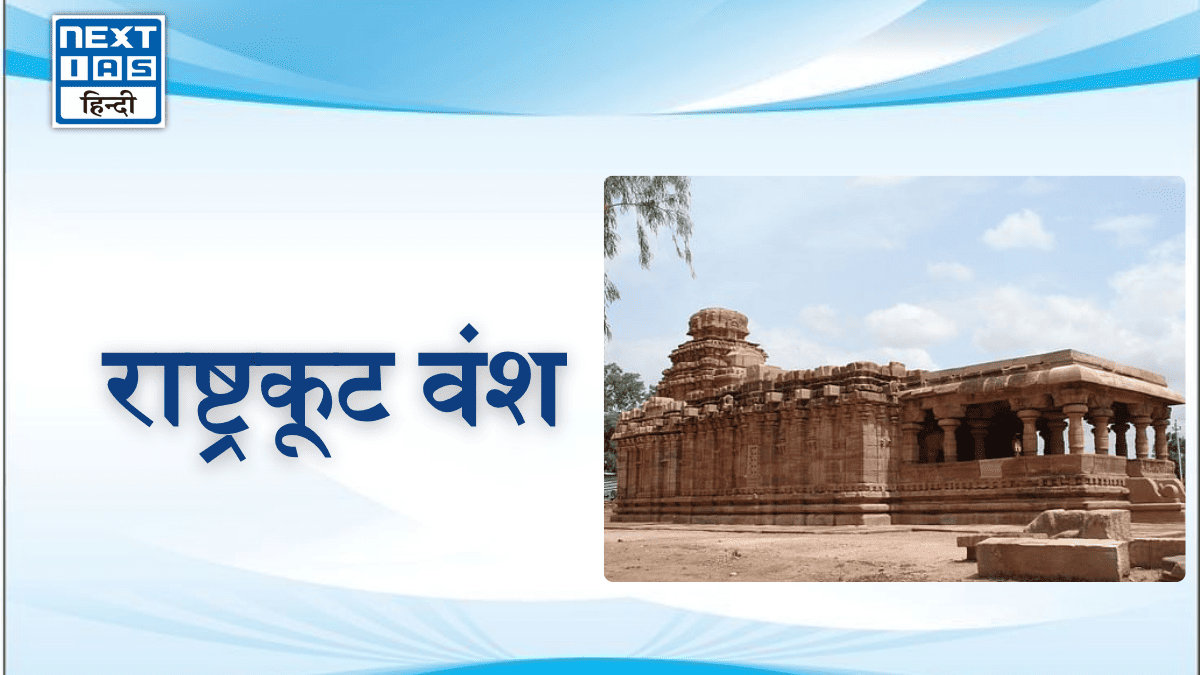भारत में जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जो अहिंसा, सत्य और त्याग को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग मानता है। इसकी विशेषता इसके गहरे सांस्कृतिक, दार्शनिक और नैतिक प्रभाव में निहित है, जिसने भारतीय जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित किया है जैसे कि कला, स्थापत्य और व्यापार। यह लेख जैन धर्म का विस्तृत अध्ययन करने का उद्देश्य रखता है, जिसमें इसके उद्भव, प्रसार, सिद्धांत और शिक्षाएं, संप्रदाय, तथा भारतीय समाज में इसके योगदान और अन्य संबंधित पहलुओं को शामिल किया गया है।
जैन धर्म के बारे में
- जैन धर्म, विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति भारत में लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, हालांकि इसके मूल इससे भी पहले के समय से जुड़े हुए हैं।
- इस धर्म की स्थापना वर्धमान महावीर ने की थी, जो जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म में अहिंसा (हिंसा का पूर्ण त्याग), त्याग और आत्म-संयम को आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग बताया गया है।
- जैन दर्शन का मूल आधार है कि आत्मा शाश्वत है, और कर्म ही किसी जीव की गति और भविष्य को निर्धारित करता है।
- जैन धर्म का कठोर नैतिक अनुशासन, विचार, वचन और कर्म में अहिंसा की गहन भावना, और इसका तपस्वी स्वरूप भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर अत्यंत प्रभावशाली रहा है।
जैन तीर्थंकर
- जैन परंपरा के अनुसार, कुल 24 तीर्थंकर (अर्थात् “संसर रूपी धारा को पार कराने वाले”) हुए हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर थे।
- यह उल्लेखनीय है कि दो जैन तीर्थंकरों—ऋषभदेव और अरिष्टनेमि—के नाम ऋग्वेद में भी पाए जाते हैं, जो जैन धर्म की प्राचीनता की पुष्टि करते हैं।
| क्रम संख्या | नाम | प्रतीक |
|---|---|---|
| 1 | ऋषभदेव | बैल |
| 2 | अजीतनाथ | हाथी |
| 3 | सम्भवनाथ | घोड़ा |
| 4 | अभिनंदननाथ | बंदर |
| 5 | सुमतिनाथ | कुरल (एक पक्षी) |
| 6 | पद्मप्रभु | लाल कमल |
| 7 | सुपार्श्वनाथ | स्वस्तिक |
| 8 | चंद्रप्रभु | चंद्रमा |
| 9 | सुविधिनाथ | मगरमच्छ |
| 10 | शीतलनाथ | श्रीवत्स |
| 11 | श्रेयांसनाथ | गैंडा |
| 12 | वासुपूज्य | भैंस |
| 13 | विमलनाथ | सूअर |
| 14 | अनंतनाथ | बाज (फाल्कन) |
| 15 | धर्मनाथ | वज्र |
| 16 | शांतिनाथ | हिरण |
| 17 | कुंतुनाथ | बकरा |
| 18 | अर्णनाथ | मछली |
| 19 | मल्लिनाथ | जल-पात्र |
| 20 | मुनिसुव्रतनाथ | कछुआ |
| 21 | नेमिनाथ | नीला कमल |
| 22 | अरिष्टनेमि | शंख |
| 23 | पार्श्वनाथ | सर्प |
| 24 | महावीर | सिंह |
प्रथम तीर्थंकर (ऋषभदेव)
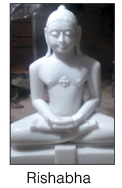
- प्रतीक: बैल
- जन्म स्थान: अयोध्या
- मोक्ष स्थान: कैलाश पर्वत
- पत्नियाँ: सुनंदा और सुमंगला
- माता-पिता: नाभि (पिता); मरुदेवी (माता)
तेईसवें तीर्थंकर (पार्श्वनाथ)

- प्रतीक: सर्प
- जन्म: 9वीं – 7वीं शताब्दी ई.पू. (वाराणसी)
- मृत्यु: 8वीं या 7वीं शताब्दी ई.पू. (शिखरजी); पार्श्वनाथ (पारसनाथ) पर्वत, गिरिडीह, झारखंड
- पत्नी: प्रभावती या कभी विवाह नहीं किया
- माता-पिता: अश्वसेन (पिता); वामादेवी (माता)
- उनकी चार मूल शिक्षाएं (चतुर्थी) थीं:
- अहिंसा (हिंसा न करना )
- सत्य (झूठ न बोलना)
- अस्तेय (चोरी न करना)
- अपरिग्रह (संपत्ति का त्याग)
- महावीर स्वामी ने इन चार शिक्षाओं को अपनाया तथा एक और शिक्षा जोड़ी —
चौबीसवें तीर्थंकर (वर्धमान महावीर)

- प्रतीक: सिंह
- जन्म: 540 ई.पू. कुंडग्राम, वैशाली (बिहार) के निकट
- मृत्यु: पावापुरी, बिहार; 468 ई.पू.
- पत्नी: यशोदा
- माता-पिता: सिद्धार्थ (पिता; ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के मुखिया); त्रिशला (माता)
- महावीर ने यशोदा (समरवीर राजा की पुत्री) से विवाह किया था और उनकी एक पुत्री हुई — प्रियदर्शना, जिसके पति जमालि उनके प्रथम शिष्य बने।
- 30 वर्ष की आयु में, पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने परिवार का त्याग कर सन्यास ग्रहण किया और सत्य की खोज में निकल पड़े।
- उनके साथ मक्काली घोषाल भी थे, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण घोषाल ने उन्हें छोड़ दिया और आजीवक संप्रदाय की स्थापना की।
- 42 वर्ष की आयु में, जंभिकग्राम में सल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका नदी के तट पर, महावीर ने कैवल्य या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया।
- कैवल्य के माध्यम से उन्होंने दुख और सुख पर विजय प्राप्त की।
- इसके बाद उन्हें महावीर (बहादुर), जितेन्द्रिय (अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला), केवलिन (पूर्ण विद्वान), निगंठ (सभी बंधनों से मुक्त) और अरिहंत (धन्य व्यक्ति) कहा जाने लगा और उनके अनुयायियों को जैन नाम दिया गया।
- उन्होंने अपना प्रथम उपदेश पावा में अपने शिष्यों को दिया, जिन्हें गंधार कहा गया, और वहीं पर उन्होंने जैन संघ की स्थापना की।
वर्धमान महावीर की शिक्षाएँ
- ईश्वर में विश्वास: उन्होंने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। उन्होंने सृष्टिकर्ता के रूप में सर्वशक्तिमान की शक्ति को नकार दिया।
- अहिंसा: उनका विश्वास था कि प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है, इसलिए उन्होंने पूर्ण अहिंसा का पालन करने की शिक्षा दी। इसी कारण से जैन धर्म के अनुयायी पैदल चलते हैं, पानी को छानकर पीते हैं, और मुख पर कपड़ा बांधते हैं ताकि किसी सूक्ष्म जीव की भी हानि न हो।
- मोक्ष की प्राप्ति: उन्होंने तपस्या और स्वेच्छा से भूख से मृत्यु द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया।
- मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने त्रिरत्न यानी सम्यक श्रद्धा (सही विश्वास), सम्यक ज्ञान (सही ज्ञान), सम्यक आचरण (सही व्यवहार) का पालन आवश्यक बताया।
- जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं: उन्होंने सामाजिक समानता और वैश्विक बंधुत्व पर बल दिया और जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया।
- कर्म का सिद्धांत: उन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास किया।
| Note: 1. महावीर के अनुसार, व्यक्ति पिछले जन्म में किए गए पाप या पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च या निम्न वर्ण में जन्म लेता है। 2. महावीर ने चांडाल जैसे निम्न वर्ण के लोगों में भी मानवीय मूल्य देखे।उनके अनुसार, निचली जातियों के लोग भी शुद्ध और पुण्यपूर्ण जीवन जीकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। |
जैन धर्म के सिद्धांत
जैन धर्म के पाँच प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं:
- अहिंसा – हिंसा न करना
- सत्य – झूठ न बोलना
- अस्तेय – चोरी न करना
- अपरिग्रह – संपत्ति का संग्रह न करना
- ब्रह्मचर्य – इंद्रियों पर संयम (संयम का पालन करना)
| Note: 1. जैन धर्म में अहिंसा या सभी जीवों को क्षति न पहुँचाने को सर्वोपरि माना गया है। 2. उन्होंने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें जिन (जिनेंद्र) से निम्न स्थान पर रखता है। 3. बौद्ध धर्म की तरह वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता। 4. इसके अनुयायियों को युद्ध में भाग लेने या कृषि करने से मना किया गया है, क्योंकि दोनों कार्यों में जीवों की हिंसा हो सकती है। – इसलिए जैन धर्म के अनुयायी मुख्यतः व्यापार एवं वाणिज्य तक सीमित रहे। 5. इसका मुख्य उद्देश्य है — सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना। – इस मुक्ति के लिए कोई अनुष्ठान या कर्मकांड आवश्यक नहीं है। |
जैन धर्म के त्रिरत्न (Triratnas of Jainism)
त्रिरत्न या तीन रत्न, जैन धर्म के वे मूल सिद्धांत हैं जो एक अनुयायी को आध्यात्मिक मुक्ति (मोक्ष) की ओर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं:
- सम्यक ज्ञान (Right Knowledge): इसका अर्थ है वास्तविकता, आत्मा और ब्रह्मांड की सच्ची समझ रखना।
- इसमें आत्मा, कर्म और जन्म-मरण के चक्र (संसार) के मूल सत्य को पहचानना शामिल है।
- सम्यक दर्शन (Right Faith): सम्यक दर्शन का तात्पर्य है जैन धर्म की शिक्षाओं पर गहरा विश्वास और आस्था।
- यह सत्य के सिद्धांतों और तीर्थंकरों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर अडिग विश्वास को दर्शाता है।
- सम्यक चरित्र (Right Conduct): यह नैतिक अनुशासन और नैतिक शुद्धता के बारे में है।
- इसमें आत्मा को शुद्ध करने और कर्म बंधन को कम करने के लिए पांच व्रतों (अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह) का पालन करना शामिल है।
जैन धर्म के दो संप्रदाय
जैन धर्म के दो संप्रदाय है श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर वे हैं जो सफेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर वे हैं जो खुद को नग्न रखते हैं।
| विषय | श्वेतांबर और दिगंबर के बीच अंतर |
|---|---|
| नग्नता का अभ्यास | दिगंबर संन्यास पथ और मोक्ष की प्राप्ति के लिए नग्नता के अभ्यास को एक अनिवार्य शर्त मानते हैं। हालांकि, श्वेतांबर यह मानते हैं कि पूर्ण नग्नता का अभ्यास मोक्ष प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं है। |
| महिलाओं की मुक्ति | दिगंबर यह मानते हैं कि महिलाओं में मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक वज्र देह और दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव होता है। दूसरी ओर, श्वेतांबर विपरीत मत रखते हैं और यह मानते हैं कि महिलाएं वर्तमान जीवनकाल में ही मोक्ष प्राप्त करने में सक्षम हैं। |
| सर्वज्ञ व्यक्ति के लिए भोजन | दिगंबरों के अनुसार, एक साधु जब केवल या ज्ञान, अर्थात सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है, तो उसे भोजन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन श्वेतांबर इस मत को नहीं मानते। |
| चरित्र और पुराण | श्वेतांबर महान आचार्यों की जीवनी के लिए ‘चारित्र’ शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि दिगंबर इसके लिए ‘पुराण’ शब्द का उपयोग करते हैं। |
| विहित साहित्य | श्वेतांबर वर्तमान में उपलब्ध बारह अंगों और सूत्रों जैसे आगमिक साहित्य की प्रामाणिकता और पवित्रता में विश्वास रखते हैं। दूसरी ओर, दिगंबर यह मानते हैं कि मूल ग्रंथ बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे। दिगंबर आचार्य स्थूलभद्र के नेतृत्व में आयोजित पहले संगीति के कार्यों और अंगों के पुनर्गठन को भी स्वीकार नहीं करते। |
जैन धर्म के मुख्य अनुयायी
- बिम्बिसार (लगभग 558-491 ईसा पूर्व), अजातशत्रु (लगभग 492-460 ईसा पूर्व), और उदायिन (लगभग 460-440 ईसा पूर्व) संरक्षक के रूप में।
- दक्षिण भारत में, गंग वंश, कदंब वंश, अमोघवर्ष (राष्ट्रकूट वंश)।
- कर्नाटक (चंद्रगुप्त मौर्य)।
जैन संगीति (Jain Councils)
| संगीति | स्थान एवं अध्यक्ष | परिणाम |
|---|---|---|
| प्रथम जैन संगीति (300 ई.पू.) | स्थान: पाटलिपुत्र अध्यक्ष: स्थूलभद्र सरंक्षण: चंद्रगुप्त मौर्य | 14 परवों के स्थान पर 12 अंगों का संकलन |
| द्वितीय जैन संगीति (512 ई.) | स्थान: वल्लभी अध्यक्ष: देववृद्धिगणि क्षमाश्रमण सरंक्षण: – | 12 अंगों और 12 उपांगों का अंतिम संकलन |
जैन साहित्य
- जैनों का पवित्र साहित्य प्राकृत की अर्धमागधी रूप में लिखा गया था।
- इन ग्रंथों का संकलन अंततः छठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ, जो एक महान शिक्षा केंद्र था।
- जैनों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाने से इस भाषा और इसके साहित्य के विकास को प्रोत्साहन मिला: 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिचरण, 6 छेदसूत्र, 4 मूलसूत्र, और 2 सूत्र ग्रंथ।
- पूर्व/परव 12 अंगों का हिस्सा हैं और ये महावीर के उपदेशों के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं।
- कल्पसूत्र (संस्कृत) भद्रबाहु द्वारा रचित है और इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ वर्णित हैं, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की, जिनमें महावीर का निर्वाण भी शामिल है।
- भद्रबाहु चरित, रत्ननंदी द्वारा लगभग 1450 ईस्वी में रचित।
- परिशिष्ट पर्व (त्रिषष्टिशलाका पुरुष का परिशिष्ट) हेमचंद्र द्वारा रचित।
जैन धर्म का प्रसार
- बौद्ध धर्म के विपरीत, जैन धर्म मुख्यतः भारत तक ही सीमित रहा। यह दक्षिण और पश्चिम भारत में फैला, जहाँ ब्राह्मण धर्म की पकड़ कमजोर थी।
- एक बाद की परंपरा के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य (322–298 ई.पू.) को कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय दिया जाता है।
- कहा जाता है कि महावीर की मृत्यु के 200 वर्ष बाद मगध में एक भीषण अकाल पड़ा, जो बारह वर्षों तक चला।
- इस अकाल से बचने के लिए, कई जैन मुनि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चले गए, जबकि शेष मगध में स्थुलभद्र के नेतृत्व में रह गए।
- जैन धर्म का प्रसार चौथी शताब्दी ई.पू. में उड़ीसा के कलिंग क्षेत्र तक हुआ।
- पहली शताब्दी ई.पू. में कलिंग के राजा खारवेल ने इसे संरक्षण दिया। उन्होंने मगध और आंध्र के राजाओं को पराजित किया था।
- दूसरी और पहली शताब्दी ई.पू. में यह तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों तक भी पहुँच गया।
- बाद की शताब्दियों में यह मालवा, राजस्थान और गुजरात तक फैल गया।
- आज भी इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जैन रहते हैं, जो मुख्यतः व्यापार और वाणिज्य में संलग्न हैं।
भारतीय भाषाओं में जैन धर्म का योगदान
- कई क्षेत्रीय भाषाएँ प्राकृत भाषाओं से उत्पन्न होकर विकसित हुईं, विशेष रूप से शौरसेनी से, जिससे मराठी भाषा का विकास हुआ।
- जैनों ने अपभ्रंश में प्रारंभिक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ कीं और उसकी पहली व्याकरण की रचना की।
- जैन साहित्य का एक बड़ा भाग अभी भी पांडुलिपि रूप में है, जिसे अभी प्रकाशित नहीं किया गया है, और ये राजस्थान तथा गुजरात के जैन तीर्थों में पाए जाते हैं।
- प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान जैनों ने संस्कृत का भी भरपूर उपयोग किया और कई संस्कृत ग्रंथों की रचना की।
- उन्होंने कन्नड़ भाषा के विकास में भी योगदान दिया और इस पर व्यापक रूप से लिखा।
जैन वास्तुकला
प्राचीन काल में जैन कला बौद्ध कला जितनी समृद्ध नहीं थी, लेकिन मध्यकाल में जैन धर्म ने कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:
- गुफाएँ (गुम्फाएँ): हाथीगुफा, बाघगुफा आदि – उदयगिरि (भुवनेश्वर) और खंडगिरि (उड़ीसा), खारवेल द्वारा निर्मित।
- मंदिर: लगभग 90 प्रतिशत जैन मंदिर किसी एक समृद्ध व्यक्ति द्वारा दान में दिए गए।
- ये मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और उत्कृष्ट निर्माण कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं।
- प्रसिद्ध जैन मंदिर:
- दिलवाड़ा मंदिर, विमलवसाही मंदिर और तेजपाल मंदिर – माउंट आबू (राजस्थान)
- गिरनार और पालिताना (गुजरात)
- पावापुरी मंदिर और राजगृह मंदिर (बिहार)
- गोमतेश्वर / बाहुबली की मूर्ति: श्रवणबेलगोला (कर्नाटक) में स्थित – यह एक भव्य मूर्ति है और जैन स्थापत्य का अद्वितीय उदाहरण है।
- जैन स्तंभ (टॉवर): चित्तौड़ के किले में स्थित जैन टॉवर वास्तुकला की एक और अद्भुत मिसाल है।
- अनेक ताड़पत्र पांडुलिपियाँ लिखी गईं, जिनमें से कुछ पर स्वर्ण धूल से सजावट भी की गई।
- इस परंपरा ने चित्रकला की एक नई शैली को जन्म दिया, जिसे “पश्चिमी भारतीय चित्रकला शैली” कहा जाता है।
जैन धर्म का व्यापार में योगदान
- जैन धर्म ने अपने अनुयायियों को युद्ध और यहां तक कि कृषि करने से भी मना किया, क्योंकि इन दोनों में जीवों की हत्या होती है।
- इसलिए, जैनों ने खुद को व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों तक सीमित कर लिया।
- व्यापार से होने वाले लाभ ने उन्हें बैंकर, पैसे बदलने वाले, आदि के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया।
- ये लाभ फिर से वाणिज्यिक प्रयासों में लगाया जाता था, जिससे उनकी भौतिक समृद्धि और आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि हुई।
- जैन प्राचीन काल से प्रसिद्ध व्यापारी रहे हैं। मध्यकाल में, उन्होंने इस पेशे में निरंतरता बनाए रखी और समृद्ध हुए। गुजरात के जगदू को तेरहवीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध जैन व्यापारी माना जाता है।
- जैन, अन्य भारतीय व्यापारियों की तरह, व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार से लाभान्वित हुए। उनकी मजबूत उपस्थिति आगरा में भी थी, जो उत्तर भारतीय व्यापार का केंद्र था। इसके अलावा, वे उत्तर भारत के दो अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक बाजारों: लाहौर और मुल्तान में भी अच्छे प्रतिनिधित्व के साथ मौजूद थे।
- वे पैसे उधार देने वाले बन गए, व्यापारी, शासक, और राज्य के अधिकारियों को भारी रकम उधार देते थे।
- सत्रहवीं शताब्दी में, जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ सामान्यतः तरल पूंजी से प्रभावित होती थीं, तो वे भारतीय उधारी देने वालों, जिनमें जैन भी शामिल थे, से अपने भारतीय भूमि पर खरीदारी के लिए वित्तीय मदद लेती थीं।
- इससे जैनों और अन्य भारतीय व्यापारियों को अतिरिक्त लाभ हुआ।
जैन धर्म के सीमित प्रसार के कारण
जैन धर्म के पांच प्रमुख सिद्धांत इसके सीमित प्रसार के कारण थे, क्योंकि ये काफी कठोर थे।
- जैन धर्म में कठोर नियम और जीवन जीने के सख्त तरीके थे, जो वैश्विक स्तर पर अपनाने में कठिन थे।
- जैन धर्म ने कभी मिशनरी उत्साह के साथ प्रचार नहीं किया।
- जैन धर्म का शाकाहार और अहिंसा का सिद्धांत भी इसके सीमित प्रसार का एक कारण था।
- जैन धर्म में यहां तक कि कृषि को भी हिंसा माना जाता था, जिससे जैनों को कृषि करने की अनुमति नहीं थी।
- जैन धर्म प्राचीन कृषि आधारित समाजों में कम लोकप्रिय था, खासकर भारत में, जहाँ विशाल जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई थी।
जैन धर्म के पतन के कारण
- राजकीय संरक्षण की कमी: महान शासकों जैसे बिम्बिसार, आजातशत्रु, उदयिन, और खारवेला ने जैन धर्म को राजकीय संरक्षण दिया था, लेकिन बाद में बौद्ध शासकों जैसे अशोक, कनिष्क, और हरशवर्धन के प्रभाव के कारण जैन धर्म पीछे पड़ गया।
- प्रचार की कमी: जैन अनुयायी धर्म के प्रचार के प्रति गांवों और कस्बों में उत्साही नहीं थे।
- जैन धर्म की कठोरता: जैन धर्म के अनुयायी कठोर तपस्या और आत्म-निग्रह का पालन करते थे, जो सामान्य लोगों को अप्रिय था और वे इससे अलग हो गए।
- फिरकापंथी मतभेद: भद्रबाहु के अनुयायी महावीर के उपदेशों का पालन करने का समर्थन करते थे, जबकि स्थुलभद्र के अनुयायी जैन धर्म की कठोरता को कम करने का पक्ष लेते थे, जिससे जैन समाज में विभाजन हुआ।
- अस्पष्ट दार्शनिकता: जीव, अजीव, पुड्गल, स्यादवाद आदि के सिद्धांत आम लोगों के लिए समझने में कठिन थे।
- बौद्ध धर्म का प्रसार: बुद्ध ने अत्यधिक कठिनाइयों का विरोध किया और ‘मध्यम मार्ग’ की प्रस्तावना की, जिसने बौद्ध धर्म को सरल और स्वीकार्य बना दिया।
निष्कर्ष
जैन धर्म, जो अहिंसा, आत्म-अनुशासन और आत्मिक मुक्ति की प्राप्ति पर गहरा जोर देता है, ने भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। अपने कठोर सिद्धांतों और उपमहाद्वीप के बाहर सीमित प्रसार के बावजूद, जैन धर्म ने भारतीय दर्शन, कला, वास्तुकला और व्यापार पर अमिट छाप छोड़ी है। इसके प्रभाव को भाषा, साहित्य और नैतिक प्रथाओं में देखा जा सकता है। भले ही जैन धर्म ने वैश्विक स्तर पर व्यापक प्रसिद्धि प्राप्त न की हो, लेकिन इसके भारत में निरंतर प्रभाव ने इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रमाणित किया है।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
जैन धर्म के संस्थापक कौन थे?
वर्धमाना महावीर को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में माना जाता है, जो 24वें तीर्थंकर थे।
महावीर के मुख्य उपदेश क्या थे?
महावीर के मुख्य उपदेश अहिंसा, सत्य और त्याग के सिद्धांतों के चारों ओर केंद्रित थे।
जैन धर्म के सीमित प्रसार के कारण क्या थे?
जैन धर्म द्वारा प्रचारित कठोर नियमों व जीवनशैली के कारण इसे सीमित प्रसार प्राप्त हुआ।
Read this article in English: Jainism: Doctrines, Sects, Contributions & More
सामान्य अध्ययन-1