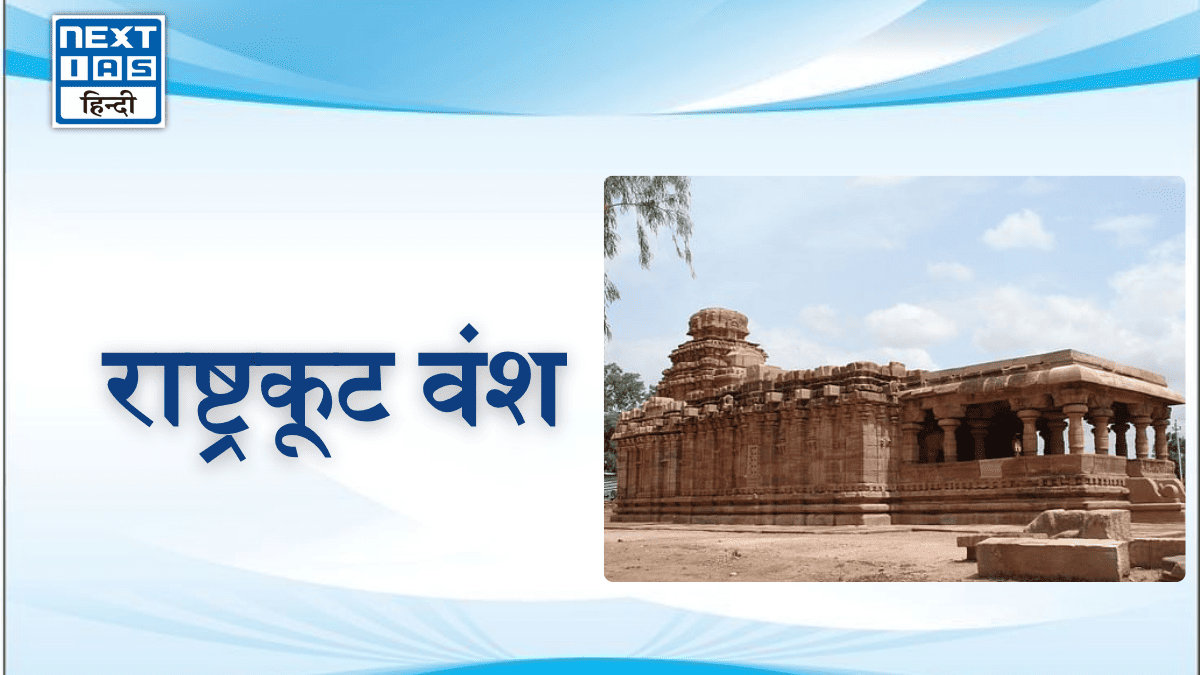सम्राट अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था, जिसने 268 ई.पू. से 232 ई.पू. तक शासन किया। अशोक एक निर्दयी विजेता से बौद्ध धर्म के समर्थक में हुए अद्वितीय परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसने न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को, बल्कि अन्य देशों को भी गहराई से प्रभावित किया। यह लेख अशोक के सत्ता में आने, उसके बौद्ध धर्म में रूपांतरण, कलिंग युद्ध का प्रभाव, उसके धम्म और शिलालेखों तथा इतिहास में उसकी स्थायी विरासत का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करता है।
सम्राट अशोक
- अशोक, जिसे अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया।
- अशोक एक भयंकर योद्धा से एक धर्मनिष्ठ बौद्ध में बदल गया।
- कलिंग युद्ध में हुए भारी नरसंहार और पीड़ा को देखने के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और इसकी शिक्षाओं को एशिया भर में फैलाया।
- उसने सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु स्तंभों और चट्टानों पर आदेश खुदवाए।
- बौद्ध धर्म के प्रचार और उसके संदेश को फैलाने के प्रयासों से भारत और दूसरे देशों की संस्कृति एवं धर्म पर उसका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
अशोक का उदय
- अशोक का उदय मौर्य साम्राज्य की शक्ति और परिवर्तन की एक प्रभावशाली कहानी है।
- 268 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक ने मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभाली। प्रारंभ में उसने एक कुशल और दृढ़ सैन्य नेता के रूप में अपने गुणों को प्रदर्शित किया और आक्रामक अभियानों के माध्यम से साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में अहम भूमिका निभाई।
- अशोक की सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपलब्धि कलिंग की विजय थी, जिसने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से गहराई से झकझोर दिया। युद्ध के दौरान हुए भारी जनसंहार और पीड़ा को देखकर उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया।
- इस क्षण ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा व नैतिक शासन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया।
- अशोक के धर्म परिवर्तन ने उसकी नीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, जो बौद्ध सिद्धांतों को फैलाने, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने और नैतिक शासन को लागू करने पर केंद्रित था।
- एक विजेता से लोककल्याणकारी सम्राट के रूप में उसका यह परिवर्तन भारतीय इतिहास के सबसे सम्माननीय शासकों में शामिल करता है।
- बौद्ध धर्म के प्रचार और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अपने शिलालेखों के माध्यम से नैतिक संदेशों के प्रसार ने अशोक को एक अमिट ऐतिहासिक विरासत प्रदान की।
अशोक का कलिंग युद्ध
- अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े, लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध था ।
- यह युद्ध उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और वह उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध बन गया।
कलिंग युद्ध का प्रभाव
- कलिंग, भूमि और समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत के मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए इसे मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना अशोक के लिए जरुरी हो गया।
- युद्ध के विनाश और नतीजों से लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। जब अशोक ने खुद यह तबाही देखी, तो उसे पश्चाताप होने लगा।
- यद्यपि कलिंग का विलय पूरा हो गया था, लेकिन अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को अपनाया और युद्ध और हिंसा का त्याग कर दिया।
- उसने बल और हिंसा के बजाय धम्म या धर्म द्वारा शासन करने की नीति अपनाई।
- दूसरे शब्दों में, भेरी घोष की जगह धम्म घोष ने ले ली। इसका वर्णन तेरहवें प्रमुख शिलालेख में किया गया है।
- अशोक ने अपने देशवासियों, जनजातीय लोगों और सीमावर्ती राज्यों से वैचारिक अपील की। सुने लोगों से कहा गया कि वे राजा को अपना पिता मानकर उसकी आज्ञा मानें और उस पर भरोसा करें।
- अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे सम्राट की धम्म की विचारधारा को समस्त प्रजा के बीच प्रचारित करें।
- अशोक ने अब विदेशी भूमि को सैन्य विजय के लिए वैध क्षेत्र नहीं माना। अशोक ने उन्हें वैचारिक रूप से जीतने की कोशिश की।
- उन्होंने पश्चिम एशिया और ग्रीस में शांति के राजदूत तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मिशनरी भेजे।
- एक प्रबुद्ध शासक के रूप में, अशोक ने प्रचार के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश की।
- यह मानना गलत होगा कि कलिंग युद्ध ने अशोक को पूरी तरह शांतिवादी बना दिया था। उसने सभी परिस्थितियों में शांति के लिए शांति नीति का पालन नहीं किया।
- अशोक ने कलिंग की विजय के बाद उसके क्षेत्रों को अपने पास रखा और उन्हें अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। उसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनायी गई विशाल सेना को भंग नहीं किया।
- अशोक ने राजुकों को नियुक्त किया, जिनके पास आवश्यकता पड़ने पर लोगों को पुरस्कृत और दंडित करने का अधिकार था।
- कंधार शिलालेख में उल्लेख है कि अशोक की नीति का शिकारियों और मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, उन्होंने जानवरों की हत्या छोड़ दी और संभवतः एक स्थायी कृषि जीवन अपनाया।
अशोक का धम्म
- अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी जिसका उद्देश्य लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना था। यह बौद्ध धर्म का पर्याय नहीं था बल्कि मनुष्य की गरिमा और मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था।
- अशोक ने महिलाओं सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म-महामंत्रों की स्थापना की।
- अशोक का धम्म संकीर्ण नहीं था बल्कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था।
- अशोक के धम्म की विषय-वस्तु उसके शिलालेखों में पाई जाती है और धम्म का सार नीचे दिए गए तरीके से समझा जा सकता है:
- पशु बलि और उत्सव समारोहों पर रोक लगाना और महंगे और निरर्थक समारोहों व अनुष्ठानों से बचना।
- सामाजिक कल्याण की दिशा में प्रशासन का कुशल संगठन।
- पशुओं के प्रति सम्मान और अहिंसा, रिश्तेदारों के प्रति शिष्टाचार और ब्राह्मणों, श्रमणों आदि को स्वतंत्रता।
- स्वामी द्वारा नौकरों के साथ और सरकारी अधिकारियों द्वारा कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार।
- माता-पिता की आज्ञा का पालन करना और ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना।
- सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता।
- भेरी घोष (युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि) की जगह धम्म घोष (शांति की ध्वनि) की स्थापना की गई, यानी युद्ध के बजाय धम्म के माध्यम से विजय।
- उन्होंने अनुष्ठानों को अस्वीकार किया, खासकर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को।
- अशोक ने लोगों को “जीयो और जीने दो” का संदेश दिया। उसकी शिक्षाओं का उद्देश्य परिवार की संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करना था।
- उसका मानना था कि अगर लोग अच्छा व्यवहार करेंगे, तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा, न कि निर्वाण, जैसा कि बौद्ध मानते थे।
- इससे यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का समर्थन करते हुए भी, एक सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों और धार्मिक निष्पक्षता को बनाए रखा। उन्होंने किसी एक धर्म के पक्ष में पक्षपात न करते हुए सभी धार्मिक परंपराओं के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया।
अशोक के शिलालेख
अशोक के शिलालेखों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
वृहद् शिलालेख
वृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी और ये आठ स्थानों पर पाए गए:
- मानसेहरा,
- शाहबाजगढ़ी,
- कलसी,
- धौली,
- जौगड़ा,
- सोपारा,
- गिरनार, और
- येरगुड्डी।
लघु शिलालेख
- लघु शिलालेख मास्की, गुर्जरा आदि स्थानों पर पाए गए।
- अशोक का नाम केवल लघु शिलालेखों की प्रतियों में दिखाई देता है, जबकि अन्य सभी शिलालेखों में उसका उल्लेख देवानाम्पिय के रूप में किया गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय।
स्तंभ शिलालेख
- स्तंभ शिलालेखों की संख्या सात थी और ये छह स्थानों पर पाए गए:
- दिल्ली-टोपरा,
- दिल्ली-मेरठ,
- लौरिया-अरेराज,
- लौरिया-नंदनगढ़,
- प्रयाग, और
- रामपुरवा।
| अशोक के 14 वृहद शिलालेख | |
|---|---|
| शिलालेख संख्या | विषयवस्तु |
| शिलालेख 1 | पशु वध पर प्रतिबंध। पशु बलि वाले उत्सवों और त्योहारों के आयोजन पर प्रतिबंध। अशोक की रसोई भी प्रभावित हुई, जहां भोजन के लिए केवल दो मोर और एक हिरण को मारा जाता था, एक प्रथा थी, जिसे वह समाप्त करना चाहता था। |
| शिलालेख 2 | मनुष्यों और पशुओं की देखभाल की व्यवस्था। इसमें दक्षिण भारत के चोल, पांड्य जैसे राज्यों का वर्णन है। |
| शिलालेख 3 | ब्राह्मणों के प्रति उदारता। |
| शिलालेख 4 | भेरीघोष (युद्ध द्वारा विजय) के बजाय धम्मघोष (धर्म द्वारा विजय) को प्राथमिकता। |
| शिलालेख 5 | दासों के प्रति नीति की चिंता। |
| शिलालेख 6 | जनकल्याण की योजनाएँ और उपाय। |
| शिलालेख 7 | सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की अपील। |
| शिलालेख 8 | अशोक की बोध गया और बोधि वृक्ष की पहली धम्मयात्रा का वर्णन |
| शिलालेख 9 | लोकप्रिय धार्मिक समारोहों की निंदा। धम्म से संबंधित समारोहों पर ज़ोर। |
| शिलालेख 10 | यश और प्रसिद्धि की चाह की निंदा। धम्म की लोकप्रियता पर बल। |
| शिलालेख 11 | धम्म के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन। |
| शिलालेख 12 | विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की अपील और निर्देश। |
| शिलालेख 13 | अशोक की कलिंग पर विजय और युद्ध के बाद की करुणा का उल्लेख। |
| शिलालेख 14 | देश के विभिन्न भागों में उत्कीर्णित अभिलेखों का वर्णन |
| कलिंग के पृथक शिलालेख (Separate Edicts – Kalinga) | |
|---|---|
| शिलालेख | विषयवस्तु |
| शिलालेख 1 | अशोक ने घोषणा की: “सभी लोग मेरे पुत्र हैं।” |
| शिलालेख 2 | यहां तक कि एक व्यक्ति के लिए भी शिलालेखों का प्रचार किया जाना चाहिए। |
| अन्य शिलालेख (Other Edicts) | |
|---|---|
| शिलालेख/स्थान | विषयवस्तु |
| रानी का शिलालेख | अशोक की दूसरी रानी का उल्लेख मिलता है। |
| बाराबर गुफा शिलालेख | अजीविका संप्रदाय को बारबरा गुफा देने का वर्णन |
| कंधार द्विभाषी शिलालेख | अशोक द्वारा अपनी नीतियों पर संतोष व्यक्त करने का वर्णन |
| स्तंभलेख (Pillar Edicts) | |
|---|---|
| स्तंभलेख संख्या | विषयवस्तु |
| स्तंभलेख 1 | प्रजा की सुरक्षा |
| स्तंभलेख 2 | धर्म की परिभाषा – पापों से बचना, अनेक सद्गुण, करुणा, स्वतंत्रता आदि। |
| स्तंभलेख 3 | कठोरता, क्रूरता, क्रोध और अहंकार जैसे पापों को समाप्त करने की बात। |
| स्तंभलेख 4 | राजूकों (स्थानीय अधिकारियों) के कर्तव्यों का वर्णन। |
| स्तंभलेख 5 | जिन पशुओं को मारना वर्जित है, उनकी सूची। |
| स्तंभलेख 6 | धम्म नीति के बारे में विवरण। |
| स्तंभलेख 7 | अशोक द्वारा धम्म नीति के अंतर्गत किए गए कार्यों का विवरण; वह कहते हैं कि सभी संप्रदाय आत्म-नियंत्रण और मानसिक शुद्धता की कामना करते हैं। |
| अन्य प्रमुख स्तंभ (Other Important Pillars) | |
|---|---|
| स्तंभ/स्थान | विषयवस्तु |
| रुम्मिनदेई स्तंभ शिलालेख | अशोक की लुंबिनी यात्रा और वहाँ के करों से छूट का उल्लेख। |
| निगालीसागर स्तंभ शिलालेख (मूल रूप से कपिलवस्तु में स्थित) | इसमें उल्लेख है कि अशोक ने बुद्ध कोणकामना के स्तूप की ऊंचाई बढ़ाकर दोगुनी कर दी। |
अशोक के स्तंभ पत्थर
- मौर्य वास्तुकला में उपयोग किए गए स्तंभ पत्थरों के स्रोत विभिन्न प्रकार की सामग्री और उनके मूल स्थान को उजागर करते हैं।
- अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त चित्तीदार (स्पॉटेड) और सफेद बलुआ पत्थर (white sandstone), जो अपनी टिकाऊ प्रकृति और महीन बनावट के लिए प्रसिद्ध है, मथुरा से प्राप्त किया गया था।
- इसके विपरीत, हल्के पीले रंग का बलुआ पत्थर और क्वार्ट्जाइट (Quartzite) अमरावती से प्राप्त किए गए थे, जिससे अशोक स्तंभों को विशिष्ट रूप मिला।
- इसके अतिरिक्त, कुछ अशोक स्तंभों का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध पत्थरों और आयातित सामग्री के संयोजन से किया गया था, जो मौर्य साम्राज्य के पत्थर खनन और शिल्पकला में उन्नत ज्ञान को दर्शाता है।
- अशोक के स्तंभों में प्रयुक्त पत्थर मौर्यकालीन निर्माणकर्ताओं की तकनीकी दक्षता को उजागर करते हैं और यह भी दर्शाते हैं कि उनके निर्माण कार्यों को समर्थन देने के लिए व्यापक व्यापार नेटवर्क मौजूद थे।
अशोक के अभिलेख
- अशोक के अभिलेख, जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में चट्टानों और स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, भारत की सबसे प्राचीन पढ़ी और समझी गई लिपियों में से एक हैं।
- ये अभिलेख प्राकृत, ग्रीक, और अरामी (Aramaic) जैसी भाषाओं में लिखे गए, जो धम्म के सिद्धांतों को फैलाने के प्रति अशोक की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। धम्म में अहिंसा, नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता को प्राथमिकता दी गई थी।
- ये अभिलेख यह भी दर्शाते हैं कि अशोक ने अपने प्रजा के कल्याण, सामाजिक सद्भाव, नीतिपूर्ण शासन और पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार के प्रयास किए।
- अशोक के ये अभिलेख इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो उसके शासनकाल और कलिंग युद्ध के बाद उसके नेतृत्व में आए परिवर्तन की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
अशोक के अभिलेखों की भाषा
- अशोक को इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। वे पहले शासक थे जिन्होंने अपने अभिलेखों के माध्यम से सीधे जनता से संपर्क स्थापित किया।
- इन अभिलेखों की रचना प्राकृत भाषा में की गई थी और अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में इन्हें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था।
- हालाँकि, उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में ये अभिलेख अरमाईक भाषा और खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, जबकि अफगानिस्तान में ये अभिलेख अरमाईक और यूनानी भाषा व लिपि दोनों में लिखे गए थे।
- अशोक के ये अभिलेख उनके राजकीय जीवन, विदेश और घरेलू नीतियों, तथा उनके साम्राज्य की व्यापकता पर प्रकाश डालते हैं।
अशोक के साम्राज्य का विस्तार
- अशोक के साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश से लेकर बंगाल तक के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और दक्षिण में एक छोटे से क्षेत्र को छोड़कर पूरा भारत शामिल था।
- कश्मीर और नेपाल की घाटियाँ भी उसके साम्राज्य के विस्तार में शामिल थीं। प्रलेखित इतिहास के अनुसार, महान मौर्य सम्राट अशोक (पहली शताब्दी ईसा पूर्व) ने श्रीनगर के पुराने शहर की स्थापना की और इसका नाम पुराणधिस्थान (अब पंद्रेथान) रखा।
- अपने सारनाथ शिलालेख में, अशोक को मास्की और धर्मकोश में बौद्धशाक्य कहा गया है।
- अशोक को देवनामप्रिय, यानी देवताओं का प्रिय और पियादस्सी, यानी मनभावन रूप के रूप में भी जाना जाता था।
आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म
- अशोक ने कलिंग युद्ध के परिणामस्वरूप बौद्ध धर्म अपना लिया था।
- परंपरा के अनुसार, वह एक भिक्षु बन गया, बौद्धों को बहुत सारे उपहार दिए और बौद्ध तीर्थस्थलों की धम्म यात्राएँ कीं।
- तीसरी बौद्ध परिषद, जो 250 ईसा पूर्व में उसके शासनकाल के दौरान हुई थी, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्त तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी।
- गौतम बुद्ध की दार्शनिक व्याख्या को तीसरे पिटक, यानी अभिधम्म पिटक में संकलित किया गया था।
- दक्षिण भारत, श्रीलंका, बर्मा और अन्य देशों में मिशनरियों को भेजा गया।
- अशोक ने अपने लिए एक बहुत ही उच्च आदर्श स्थापित किया: पैतृक रिश्तेदारी (पितृत्व)। अर्थात वह अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता था।
- अशोक ने महिलाओं सहित विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म-महामात्रों को नियुक्त किया। अनुष्ठानों को भी अस्वीकार किया गया, विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को।
- अशोक ने कुछ पक्षियों और जानवरों को मारने और जानवरों का वध करने पर रोक लगाई। अशोक ने कभी निर्वाण प्राप्ति के बारे में कुछ नहीं कहा, जो बौद्ध शिक्षाओं का लक्ष्य था।
- अशोक की शिक्षाएँ सहिष्णुता पर आधारित मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थीं। उन्होंने किसी भी सांप्रदायिक आस्था का प्रचार नहीं किया।
इतिहास में अशोक का स्थान
- अशोक के नाम कई उपलब्धियाँ दर्ज हैं। वह प्राचीन विश्व के इतिहास में एक महान धर्मप्रचारक शासक थे।
- अपनी अधिकांश शिलालेखों में, उन्होंने एक धर्म, एक भाषा, और एक लिपि (ब्रह्मी) के माध्यम से देश की राजनीतिक एकता को स्थापित करने का प्रयास किया।
- हालाँकि, अशोक ने अन्य लिपियों जैसे अरामी, यूनानी और खरोष्ठी का भी सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई।
- अशोक ने अपने बौद्ध विश्वास को अपनी प्रजा पर थोपने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने गैर-बौद्ध और यहां तक कि बौद्ध विरोधी संप्रदायों को भी दान दिए।
- अशोक इतिहास में अपनी शांति नीति, आक्रामकता से दूर रहने और सांस्कृतिक विजय के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
- उन्होंने कौटिल्य के उस उपदेश का उल्टा मार्ग अपनाया जिसमें राजा को भौतिक विजय में ही तत्पर रहने को कहा गया था।
- अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से कहा कि वे विजय और आक्रामकता की नीति को त्याग दें। हालाँकि, अशोक की इस नीति का स्थायी प्रभाव उनके अधीनस्थ शासकों पर नहीं पड़ा, जिन्होंने 232 ईसा पूर्व में उनके सत्ता छोड़ने के बाद अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
- उनकी नीति पड़ोसी राज्यों को प्रभावित नहीं कर सकी, और अशोक की मृत्यु के लगभग 30 वर्षों के भीतर ही उत्तर-पश्चिमी सीमाओं पर आक्रमण प्रारंभ हो गए।
- जेम्स प्रिन्सेप पहले विद्वान थे जिन्होंने अशोक के ब्रह्मी लिपि में लिखे गए अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की।
- इन अभिलेखों में “देवानंपिय पियदस्सी” नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसे प्रारंभ में श्रीलंका का राजा समझा गया था।
- अंततः 1915 में कर्नाटक के मास्की अभिलेख ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह राजा अशोक ही था।
- अशोक से पूर्व ब्राह्मी लिपि श्रीलंका के अनुराधापुर में भी प्रयुक्त पाई गई।
- ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पत्थर की पट्टियों पर अंकित अक्षरों द्वारा समझा गया था।
- अशोक के पत्थर स्तंभ वास्तु संरचनाओं का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्र मूर्तिकला कृतियाँ हैं।
- ये स्तंभ अत्यंत चमकदार (Highly polished) और एक ही पत्थर (Monolithic) से बने हुए हैं तथा इनका शाफ्ट (shaft) ऊपर की ओर पतला होता जाता है।
- अशोक का उल्लेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित गुज्जरा लघु शिलालेख में भी मिलता है।
- बुद्ध के जन्मस्थान को चिह्नित करने के लिए, अशोक ने कुछ पवित्र पत्थर संरचनाओं के साथ रुम्मेनदेई का स्तंभ बनवाया।
- उन्होंने लुम्बिनी के धार्मिक कर को माफ कर दिया क्योंकि यह बुद्ध की जन्मस्थली थी और भूमि राजस्व दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया।
- अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक ताम्रपत्र (कॉपर प्लेट) अभिलेख, सोहगौरा ताम्रपत्र, मौर्य काल का है, जो देश में अकाल के समय अन्न भंडारण के लिए जारी किए गए शाही आदेश का उल्लेख करता है।
- अर्थशास्त्र के अनुसार, यदि किसी पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, तो उसे तलाक की अनुमति थी। अर्थात मौर्य काल में तलाक मान्य था। इसी तरह, खुशबन्द को अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ने का अधिकार था क्योंकि वह बांझ थी या व्यभिचारिणी थी।
- मौर्य शासन व्यवस्था में “पंकोदकसन्निरोधे” नामक दंड व्यवस्था थी, जो सड़कों पर कीचड़ और पानी इकट्ठा करने या गंदगी फैलाने पर लगाई जाती थी।
- अशोक के 13वें शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि उसके पाँच यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे:
- एंटिओकस द्वितीय थियोस: सीरिया का शासक।
- थुरमाया (टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फ़स): मिस्र का शासक।
- एंटाकिनी (एंटीगोनस गोनाटस): मैसेडोनिया का शासक।
- मकमास या मेगारस: साइरेन का शासक।
- एलिएरो सेंट्रो (अलेक्जेंडर एपिरस): एपिरस का शासक।
निष्कर्ष
निष्कर्षतः, अशोक महान भारतीय और विश्व इतिहास में एक परिवर्तनकारी व्यक्तित्व के रूप में सामने आता हैं, जिसके शासनकाल ने सैन्य विस्तार की नीति से नैतिक और आध्यात्मिक शासन की ओर एक गहरा मोड़ लिया। बौद्ध धर्म और धम्म के सिद्धांतों को अपनाकर अशोक ने अपने प्रशासन और नेतृत्व के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल दिया, जोकि शांति, सहिष्णुता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। अपने शिलालेखों के माध्यम से अशोक ने एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज की अपनी दृष्टि को जन-जन तक पहुँचाया, जिससे न केवल उनके समकालीनों पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म के प्रसार में अशोक के योगदान और नैतिक शासन पर दिए गए ज़ोर की गूंज आज भी सुनाई देती है, जो अशोक को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों संदर्भों में एक केंद्रीय व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करती है।
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
अशोक कौन था?
अशोक मौर्य वंश का सम्राट था, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
अशोक का धम्म क्या था?
अशोक का धम्म नैतिक और मानवीय सिद्धांतों का एक समूह था, जो अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता था।
कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा?
कलिंग युद्ध ने अशोक को गहराई से प्रभावित किया। भारी जनहानि और पीड़ा को देखकर अशोक ने हिंसा का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाकर धम्म की नीति के तहत करुणा, अहिंसा और जनकल्याण पर केंद्रित शासन शुरू किया।
अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था?
अशोक के धम्म का उद्देश्य अपने प्रजा में नैतिक मूल्यों, अहिंसा, सहिष्णुता और करुणा को बढ़ावा देना था ताकि समाज में समरसता और कल्याण स्थापित हो सके।
कलिंग युद्ध में कौन जीता?
मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में विजय प्राप्त की थी।
अशोक के शिलालेख क्या हैं?
अशोक के शिलालेख उसके द्वारा स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर खुदवाए गए अभिलेख हैं, जिनके माध्यम से उसने अपनी नीतियाँ, धम्म के सिद्धांत और जनकल्याणकारी संदेशों को प्रसारित किया।